Manuscripts ~ Bindu-Bindu Vichar, Bhag 1 (बिंदु-बिंदु विचार, भाग 1)
Jump to navigation
Jump to search
Point to Point Thought
- year
- 1967
- notes
- 14 sheets plus 2 written on reverse
- Sheet numbers showing "R" and "V" refer to "Recto and Verso".
- Published as notes 204-225 of Naye Sanket (नये संकेत).
- The transcripts below are not true transcripts, but copies from Naye Sanket (नये संकेत)
- see also
- Category:Manuscripts
sheet no original photo enhanced photo Hindi 1 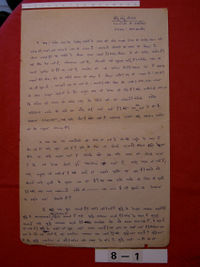
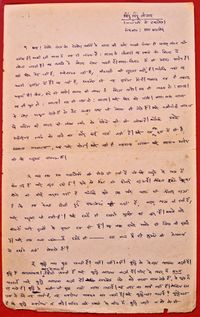
बिंदु-बिंदु विचार
(चर्चाओं से संकलित)
संकलन : रमा अरविंदNaye Sanket (नये संकेत), notes 204 - 206
- १. आह। देखो गंगा को देखो। पर्वतों से सागर की ओर भागती गंगा ही सम्यक जीवन की प्रतीक है। उसकी पूरी यात्रा में एक ही लक्ष्य हैः सागर से मिलन। वह स्वयं को विराट में खोना चाहती है। वह व्यक्ति से विराट होना चाहती है। सागर-मिलन में ही उसका आनंद है। वहां फिर भेद नहीं है, अकेलापन नहीं है, सीमाओं की क्षुद्रता नहीं है। क्योंकि वहां वह अपनी पूर्णता में है। वह नहीं है, इसलिए ही वह पूर्णता में है। जब तक वह है तब तक अपूर्ण है। मित्र, ऐसे ही बनो। सागर की खोज में सरिता बनो। एक ही लक्ष्य होः सागर। एक ही धुन होः सागर। एक ही गीत होः सागर। और फिर बहे चलो। प्राण जब सागर के लिए आकुल होते हैं तो पैर उसका पथ भी खोज ही लेते हैं। और भलीभांति जानना कि सरिता की सागर की खोज स्वयं को खोने की ही खोज है। क्योंकि उसके अतिरिक्त स्वयं को पाने का और कोई मार्ग नहीं है। और इस एक सूत्र में ही एकमात्र अध्यात्म, धर्म और योग। और यही है एकमात्र सत्य और एकमात्र आनंद जो कि मनुष्य पा सकता है।
- २. क्या हम उन मछलियों की भांति ही नहीं हैं जो कि मछुए के जाल में फंस गई हैं और तड़प रही हैं? मुझे तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। लेकिन इससे निराश होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि मुझे एक और सत्य भी दिखाई पड़ता है कि हम केवल फंसी हुई मछलियां ही नहीं हैं, वरन जाल भी हमी हैं। और मछुआ भी हमीं हैं। और इसमें ही हमारी मुक्ति का द्वार है। अपने सारे बंधनों और दुखों के सृष्टा हम ही हैं। यह सब हमारे अपने ही चित्त की सृष्टि है। और तब क्या इसमें ही- हमें तथ्य में ही मुक्ति की संभावना के दर्शन नहीं हो जाते हैं?
- ३. बुद्धि क्या कुछ जानती है? नहीं। नहीं। नहीं बुद्धि तो केवल व्याख्या करती है। बुद्धि है व्याख्याकार। बाहर के जगत में इंद्रियां जानती हैं और बुद्धि व्याख्या करती है। भीतर के जगत में हृदय जानता है और बुद्धि व्याख्या करती है। इसलिए जो उसे ज्ञाता मान लेते हैं, वे भूल में पड़ जाते हैं। बुद्धि से कभी भी कुछ नहीं जाना गया है। वह ज्ञान का मार्ग नहीं है। लेकिन इस भ्रम से कि वह मार्ग है, वह अविरोध अवश्य बन जाती है। और बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता कि बुद्धि अवरोध न बने। जीवन और स्वयं के बीच में बुद्धि खड़ी न हो तो ही
2 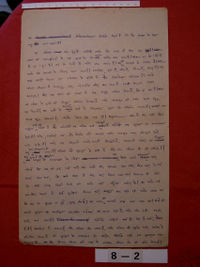
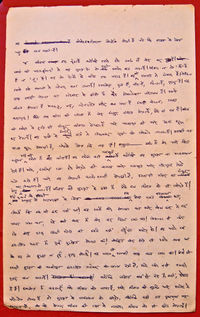
Naye Sanket (नये संकेत), notes 206 - 207 - वह संवेदनशीलता निर्मित होती है जो कि सत्य के लिए चक्षु बन जाता है।
- ४. जीवन एक कुंठा है क्योंकि हमने उसे स्वयं में बंद कर रखा है। स्वयं की चारदीवारी से वह मुक्त हो तो वही आनंद बन जाता है। जीवन न तो ‘मैं’ में है न ‘तू’ में। वह तो दोनों के बीच एक प्रवाह है। वह तो समस्त से संवाद है। लेकिन हमने उसे समस्त से विवाद बना रखा है इसलिए; दुख है, पीड़ा है, चिंता है, मृत्यु है। यह सब हमारी चेतना का अहंकार के द्वीपों में कैद हो जाने का परिणाम है। उससे जीवन हो गया है। अवरुद्ध, जड़, तरंगरहित और बन गया है, हमारा बंधन, हमारा कारागृह। जैसे एक बीज की खोल के टूटते ही अंकुर जीवंत हो जाता है और आकाश की ओर उठना शुरू कर देता है। वह भूमि के अंधेरे गर्त से निकल कर सूर्य को खोजने लगता है। उसकी वह यात्रा शुरू हो जाती है, जिसके लिए कि वह है। मनुष्य स्वयं में बंद और घिरा मनुष्य अहं की खोज में कैद बीज है। वह खोल बड़ी मजबूत है क्योंकि वह सुरक्षा का आश्वासन देती है। और, इसलिए हम उसे तोड़ने की बाजए और मजबूत और परिपुष्ट किए चले जाते हैं। और वह जितनी शक्तिशाली हो जाती है, उतना ही भीतर का अंकुर पंगु और निष्प्राण हो जाता है। जीवन को सुरक्षा के भ्रम में ऐसे हम जीवन को ही खोदते हैं। मैंने सुना है कि किसी सम्राट ने आत्म-रक्षा के लिए ऐसा भवन बनवाया था, जिसमें कि एक भी द्वार नहीं था! वह उसमें बंद हो गया था और इस द्वार से वह भीतर गया था, उसे बाद में बंद कर दिया गया था! निश्चय ही फिर उसे कोई शत्रु किसी भांति हानि नहीं पहुंचा सकते थे। वह अपने उस द्वार-रहित भवन में पूर्ण सुररिक्षत हो गया था। लेकिन बंद होते ही उसने जाना था कि यह तो सुरक्षा न हुई, मृत्यु हो गई। वह भवन ही उसकी कब्र बन गया था। ऐसे ही हमारी सुरक्षा की आकांक्षा द्वार-रहित अहंकार को जन्म देती है, और फिर वही हमारी मृत्यु बन जाता है। क्योंकि जीवन सर्व से भेद में नहीं, ऐक्य में है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन को पाना है, और जीवन की मुक्ति और आनंद से परिचित होना है तो सुरक्षा के पागलपन को छोड़ो, क्योंकि वही उस दुष्टचक्र का आधार है, जो कि अंततः जीवन की रक्षा के नाम पर जीवन को ही छीन लेता है।
3 
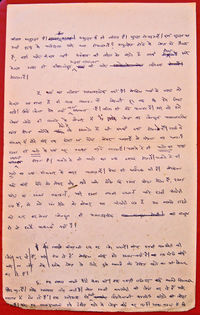
Naye Sanket (नये संकेत), notes 207 - 209 - जीवन असुरक्षा है। असुरक्षा में ही जीवन है। सुरक्षा तो जड़ता है। पूर्ण सुरक्षा का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? असुरक्षित होने के लिए जो तैयार है, वही और केवल वही अहंकार की खोल को तोड़ने में समर्थ होता और केवल उसका ही जीवनांकुर अज्ञात परमात्मा की ओर गतिमय हो पाता है।
- ५. धर्म का जीवन अव्यावहारिक नहीं है। लेकिन धर्म के सत्य को केवल उस मात्रा में ही जाना जा सकता है जितनी दूर तक कि उसे जीआ जाए। जीए बिना उसे नहीं जाना जा सकता है। जीता ही उसे जानना है। और जो उसे बिना जीए ही जानने के विचार में हैं, उनके लिए वह बिल्कुल अव्यावहारिक प्रतीत होगा क्योंकि ऐसे वे उसे समझने में भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। रजनी के अंधकार में जैसे कोई एक छोटा सा दीया लेकर चलता है तो जीतना वह चलता है उतना ही आगे के पथ पर प्रकाश पड़ने लगता है। चलने में ही आगे का पथ प्रशस्त होता है। चलने में ही मानो पथ स्पष्ट होता है। चलने से ही आगे का पथ अंधकार के बाहर आ जाता है। ऐसा ही धर्म पथ भी है। लेकिन यदि कोई दीये को लेकर लिए जाए और सोचे कि इतना छोटा दीया है, इतना थोड़ा सा इसका प्रकाश है, और इतना लंबा रास्ता है और इतनी अंधेरी रात है, तो उसे उस दीये को लेकर उस अंधेरी रात में उस रास्ते को पार कर लेना बिल्कुल ही अव्यावहारिक बात मालूम हो तो इसमें आश्चर्य नहीं है?
- ६. एक स्वप्न कभी मैंने देखा था। एक पहाड़ी रास्ते पर कोई व्यक्ति फिसल कर गिर पड़ा है। उसके आस-पास भीड़ लगी है। लोग उसकी कमजोरी की निंदा कर रहे हैं और उपहास में हंस रहे हैं। एक उपदेशक उसे ऐसी गिराने वाली कमजोरी छोड़ने की शिक्षा दे रहा है। और एक सुधारक उसे छथ्डित करने के लिए बातें कर रहा है। उसका कहना है कि
4 
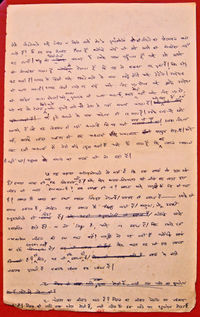
Naye Sanket (नये संकेत), notes 209 - 211 - ऐसे गिरने वाले यदि छथ्डित न किए जाएं तो वे दूसरे लोगों को भी गिरने का प्रोत्साहन बन जाते हैं। मैं यह सब देख कर हैरान हूं क्योंकि कोई भी उसे उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। भीड़ को किसी भांति पार कर मैं उसके पास पहुंचता हूं और उसे उठाने की कोशिश करता हूं तो देखता हूं कि वह तो कब का मर चुका है! फिर भीड़ छट जाती है। शायद वे किसी और गिरने वाले के पास इकट्ठे होंगे और देखेंगे। उपदेशक भी चला जाता है। शायद किसी रास्ते पर कोई और गिर पड़ा होगा और उसके उपदेश की प्रतीक्षा करता होगा। और समाज सुधारक भी चला जाता है, शायद कोई कहीं और गिर पड़ा हो, वह उसे छथ्डित किए जाने और सुधारे जाने की सेवा से नहीं बचना चाहता है। और फिर मैं उस मरे हुए व्यक्ति के पास अकेला ही रह जाता हूं। उसके हाथ पैर इतने कमजोर हैं कि यह विश्वास ही नहीं आता है कि वह कभी चला भी था! उसका गिरना नहीं, बल्कि उसका चलना ही एक आश्चर्य और चमत्कार मालूम होता है। और फिर इसी आश्चर्य में मेरी नींद खुल जाती है और मैं पाता हूं कि वह स्वप्न ही नहीं था। मनुष्य के समाज का सत्य भी तो यही है।
- ७. यह कहना अतिशयोक्ति तो नहीं है कि हम स्वयं को भूल गए हैं। हमारा जन्म ही क्या एक विस्मरण नहीं है? और फिर आत्म-विस्मरण को नींव पर खड़ा पूरा जीवन भी क्या हो सकता है? एक स्वप्न ही न? स्वप्न और जागृति में भेद ही क्या है? स्वप्न में स्वप्न का दृष्टा एकदम विस्मृत होता है। उस पर ही स्वप्न है- उसके ही समझ स्वप्न है, लेकिन वह स्वप्न में मौजूद नहीं है। वस्तुतः, तो उसकी अनुपस्थिति ही निद्रा है। क्योंकि उसके अपस्थित होते ही न तो निद्रा है, और न स्वप्न है। फिर हमारे इस तथाकथित जीवन को हम क्या कहें? जागृति तो यह नहीं है क्योंकि स्वयं का हमें स्मरण नहीं है। फिर क्या यह भी एक स्वप्न है? हां, मित्र, यह भी एक स्वप्न ही है। स्वयं के प्रति जब तक मूर्च्छा है, तब तक जीवन एक स्वप्न है।
- ८. चेतना का जीवन क्या है? चित्त का जीवन चेतना का जीवन नहीं है, चित्त की गति जब शांत होती है, तभी चित्त में उस गति का शुभारंभ होता है
5 
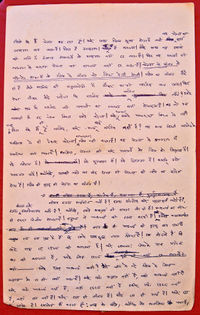
Naye Sanket (नये संकेत), notes 211 - 212 - जिसे कि मैं चेतना कह रहा हूं। और जब चित्त शून्य होता है तभी वह चेतना पूर्ण उपकरण बन जाता है। चित्त है उपकरण। वह है माध्यम। और जब वह स्वयं की गति में संलग्न हो जाता है तो उपकरण नहीं रह जाता फिर वह अपनी ही व्यस्तता के कारण चेतना का माध्यम नहीं रह जाता है। चेतना के जीवन से परिचित होना है तो चित्त के जीवन को विदा देनी होगी। चित्त का जीवन वैसे ही है जैसे मालिक की अनुपस्थिति में नौकर का ही मालिक बन जाना। फिर ऐसा नौकर कैसे चाहेगा कि मालिक वापिस लौटे? उसके मन में मालिक की वापसी का स्वागत नहीं हो सकता है। वह तो उस वापसी में हर संभव विघ्न खड़े करेगा। और उसका सबमें आधारभूत विघ्न तो यही दावा होगा कि मैं ही मालिक हूं, और अन्य कोई मालिक नहीं है? वह अन्य किसी मालिक के अस्तित्व से ही इनकार करेगा। साधारणतः चित्त यही करता है। वह चेतना के अवतरण में अवरोध बन जाता है। इसलिए, चेतना की ओर चलना है तो चित्त को विश्राम दें। उसे विराम दें। उसे शून्यता दें। उसे रिक्तता दें। अर्थात उसे अव्यस्त करें। क्योंकि, उसकी गति का बंद होना ही चेतना की गति का प्रारंभ होना है। चित्त की मृत्यु ही चेतना का जीवन है।
- ९. जीवन इतना अर्थहीन क्यों हैं? इतना यांत्रिक और जड़तापूर्ण क्यों है? इतना बेरस और उबाने वाला क्यों है? क्योंकि, हमने आश्चर्य की क्षमता खो दी है। आश्चर्य का बोध ही हमारा विलीन हो गया है। मनुष्य ने आश्चर्य की हत्या कर दी है। उसका तथाकथित ज्ञान ही आश्चर्य की मृत्यु बन गया है। हम इस भ्रम में हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है! हम सोचते हैं कि हमारे पास हर रहस्य की व्याख्या है! और स्वभावतः जिसके पास प्रत्येक बात की व्याख्या है, उसके लिए रहस्य कहां- उसके लिए आश्चर्य कहां? ऐसे ज्ञान से भरे चित्त के लिए अज्ञात तो रह ही नहीं जाता है। और जहां अज्ञात नहीं है, वहां आश्चर्य नहीं है और जहां आश्चर्य नहीं है, वहां रहस्य नहीं है और जहां रहस्य नहीं है, वहां रस नहीं है। और रस ही जीवन है। और रस ही अर्थ है। और रस ही आनंद है। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान को छोड़ो, क्योंकि जो जान लिए गया है,
6 
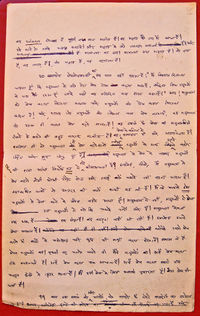
Naye Sanket (नये संकेत), notes 212 - 214 - वह इसी कारण हो गया है। मृत ज्ञानमात्र अतीत है। वह अज्ञात की बाधा है। उसे जाने दो ताकि अज्ञात आ सके। और अज्ञात के प्रति जागरण आश्चर्य है। और है परमात्मा का द्वार। परमात्मा सदा अज्ञात है। जो ज्ञात है, वह जगत है। जो अज्ञात है, वह परमात्मा है।
- १०. फ्योदोर दोस्तोवस्की का एक पात्र कहीं कहता हैः ‘मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मनुष्यता के प्रति मेरा प्रेम रोज बढ़ता जाता है, लेकिन जिन मनुष्यों के साथ में रहता हूं उनके प्रति वह प्रतिदिन कम होता जाता है।’ आह। मनुष्यता को प्रेम करना कितना आसान और मनुष्यों को प्रेम करना कितना कठिन है! और, शायद जो मनुष्यों को जितना कम प्रेम करता है, वह मनुष्यता को उतना ही ज्यादा प्रेम करने लगता है। वह स्वयं में प्रेम की अनुपस्थिति देखने से बचने की बहुत कारगर तरकीब है। वह प्रेम के कर्तव्य से पलायन है और आत्मवंचना है। इसलिए ही तो मनुष्यता से प्रेम करने वाले लोग मनुष्यों के साथ इतने कठोर, निर्दय और कूर सिद्ध हुए हैं। मनुष्यता के प्रेम के नाम पर मनुष्यों की हत्या अत्यंत निर्दोष मन से जो की जा सकती है? इसलिए, मित्रो, मैं मनुष्यता से प्रेम करने जैसी थोथी और पोच और हवाई बातें आपसे नहीं कहना चाहता हूं। तथाकथित धर्मों ने उस तरह की बातें काफी कहली हैं। मैं तो आपसे ठोस मनुष्यों से प्रेम करने के लिए कहने आया हूं। मनुष्यता से नहीं, मनुष्यों से प्रेम- उन मनुष्यों से जो कि आपके चारों ओर हैं। मनुष्यता केवल शब्द है- एक संज्ञा है। वह वस्तुतः कहीं भी नहीं है। इसलिए उससे प्रेम आसान है। क्योंकि उससे प्रेम करने में बातों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना होता है। सवाल तो है ठोस मनुष्यों का। पृथ्वी पर चलते अपने ही जैसे मनुष्यों का। उन्हें प्रेम करना एक तपश्चर्या है। उन्हें प्रेम करना एक साधना है। उन्हें प्रेम करना स्वयं एक आमूल क्रांति से गुजर जाना है। मैं उसी प्रेम के लिए आपको पुकारता हूं। वैसा प्रेम ही धर्म है।
- ११. क्या हम स्वयं को और अन्यों को सामने में दोहरे मानछथ्डों का उपयोग करते हैं?
7R 
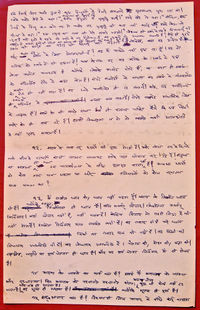
Naye Sanket (नये संकेत), notes 214 - 218 - एक ईसाई पिता अपने पुत्र से कुछ हिंदुओं के ईसाई बन जाने का सुसमाचार सुना रहा था। उसने अपने बेटे से कहाः ‘परमात्मा की दया है कि इतने हिंदुओं में सुबुद्धि आई।’ उसके बेटे ने कहाः ‘लेकिन, एक ईसाई के हिंदु बन जाने पर तो आपने यह सुबुद्धि की बात नहीं बातई थी।’ उसके पिता ने क्रोध से कहाः ‘उस उद्दार का नाम भी मेरे सामने मत लो।’ निश्चय ही स्वयं के पक्ष से जो जाता है, वह गद्दार है और दूसरे के पक्ष से जो स्वयं के पक्ष में आता है, वह सुबुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति है। ऐसे ही दुहरे मानछथ्ड के कारण दूसरे की आंख का पतंगा भी हमें दिखाई पड़ता है? लेकिन, क्या यह उचित है और क्या यह स्वयं के लिए मंगलदायी है? यह मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। यह तो प्रत्येक को स्वयं से ही पूछना है? धर्म के पथ पर यह प्रत्येक को स्वयं से पूछ लेना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जिसके मानछथ्ड दोहरे हैं, वह सदा ही स्वयं को परिवर्तित होने से बचा लेता है। दोहरे मानछथ्डों के कारण वह स्वयं के जीवन तथ्यों को कभी देख ही नहीं पाता है। वह उनसे अपरिचित ही रह जाता है और यह अपरिचय ही स्वयं के परिवर्तन से बचाव बन जाता है। दोहरे मानछथ्ड अधार्मिक चित्त के क्षण हैं। स्वयं को भी मापते समय वैसे ही मापना चाहिए जैसे कि हम किसी और को ही माप रहे हैं। इतनी निष्पक्षता न हो तो व्यक्ति कभी आत्मक्रांति से नहीं गुजर सकता है।
- १२. सत्य के नाम पर शब्दों की पूजा हो रही है। और लोग राह के किनारे लगे मील के पत्थरों को ही गंतव्य समझ कर उनके पास निवास कर रहे हैं। मनुष्य का आलस्य ही क्या इस आत्मवंचना के पीछे मूलभूत कारण नहीं है? अन्यथा शब्दों को कौन सत्य मान सकता था और प्रतिमाओं को कौन परमात्मा मान सकता था?
- १३. मैं सबीज ध्यान को ध्यान नहीं कहता हूं। ध्यान तो निर्बीज ध्यान ही है। क्योंकि वस्तुतः निर्बीजता ही ध्यान है। बीज अर्थात विचार। निर्बीजता अर्थात निर्विचार जहां विचार नहीं है, वहीं ध्यान है। लेकिन विचार तो गहरी निद्रा में भी नहीं होता है। इसलिए निर्विचार मात्र पर्याप्त नहीं है। वह नकार ही है और ध्यान किसी का नकारमात्र ही नहीं है। वह किसी की विधायक उपस्थिति भी है। वह विधायक उपस्थिति है चैतन्य की, होश की, प्रज्ञा की। इसलिए, चेतना ही ध्यान है। और यह पूर्ण चेतना निर्विचार में ही संभव है।
- १४. आत्मा को जानने का मार्ग क्या है? स्वयं में अनाम को जानना और पहचानना फिर अनात्म को पहचानते पहचानते अंततः आत्म जैसा कुछ भी शेष नहीं रह जाता है और तब ही आत्मा है। वह शून्य ही आत्मा है। क्योंकि शून्य ही पूर्ण है।
- १५. सद आचार क्या है? निश्चय ही जिस आचार के पीछे कोई वासना
7V 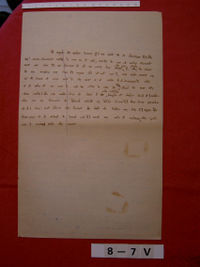

8R 
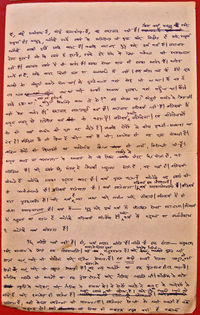
Naye Sanket (नये संकेत), notes 218 - 219 - है, कोई अभिप्राय है, कोई फलाकांक्षा है, वह सदाचार नहीं है। वैसा कर्म अशुद्ध और अपूर्ण है। अशुद्ध, क्योंकि उसमें स्वयं के अतिरिक्त भी कुछ और मिश्रित है और अपूर्ण क्योंकि इसकी पूर्ति उसके बाहर है। जब कि सदाचार शुद्ध और पूर्ण कर्म है। सदाचार ऐसा कृत्य है जो कि स्वयं में पूरा है, उसके पूरे होने के लिए भविष्य की आवश्यकता नहीं है, सदाचार स्वयं में ही आनंद है। उसका होना मात्र ही उसका आनंद है। आनंद उसमें ही है, उसके बाहर किसी फल या उपलब्धि में नहीं। एक बीहड़ वन में मैंने एक व्यक्ति को बांसुरी बजाते देखा था। उसे सुनने वाला वहां कोई भी न था। मैं वन में राह भटक गया था और उसकी आवाज सुन कर वहां पहुंचा था। मैंने पूछा थाः ‘यहां इस एकांत में बांसुरी किसलिए बजा रहे हो? ’ वह बोला थाः ‘बांसुरी बजाने के लिए ही। वही मेरा आनंद है।’ सदाचार स्वतःस्फूर्त कर्म है। सदाचार कर्म को कहता हूं। प्रतिकर्म में बाह्य जगत से उत्प्रेरित कर्म को कहता हूं। प्रतिकर्म अर्थात प्रतिक्रिया। हम प्रतिक्रियाओं को ही कर्म समझने की भूल कर बैठते हैं। जब कि दोनों की क्रियाओं का आविर्भाव भिन्न ही नहीं, विरोधी भी है। बाह्य जगत या वातावरण के आघात से जो क्रिया व्यक्ति के भीतर पैदा होती है, वह प्रतिक्रिया है। और स्वयं से, अंतस में जिसकी स्फुरणा होती है, वह कर्म है। प्रतिकर्म बांधते हैं क्योंकि उनका उदगार बाहर है। कर्म मुक्त करता है क्योंकि वह स्वयं की ही अभिव्यक्ति है। प्रतिकर्म परतंत्रता है। कर्म स्वतंत्रता प्रतिकर्म एक विवशता है कर्म आत्माभिव्यक्ति। प्रतिकर्म सदा पुनरुक्ति है। और कर्म सदा जीवन और जीवंत। प्रतिकर्म में ही जीना असदाचरण है। कर्म में- शुद्ध और पूर्ण कर्म में प्रतिष्ठित होना सदाचरण। प्रतिकर्म में मनुष्य का पतन है क्योंकि प्रतिकर्म यांत्रिक है। और कर्म में मनुष्य का ऊध्र्व विकास है क्योंकि कर्म चेतना है।
- १६. नीति धर्म नहीं है। हां, धर्म जरूर नीति है। नीति है एक ढांचा- अनुकरण और अभ्यास के लिए एक नियमावली। वह ऊपर से थोपा हुआ अनुशासन है। इसलिए नैतिक व्यक्ति मुक्त नहीं होता वरन और भी यांत्रिक और परतंत्र हो जाता है। इस भांति उसकी चेतना जाग्रत तो नहीं होती, वरन और प्रसुप्त हो जाती है। अंततः तो वह जड़ आदमी का एक पुंजमात्र ही रह जाता है। अनैतिक व्यक्ति भी आदतों का एक पुंज है और नैतिक व्यक्ति भी। अनैतिक ने माने प्रकृति के आदेश, और नैतिक ने माने समाज के। वे दोनों अपने से बाहर के आदेशों से जीते हैं और इसलिए ही परतंत्र हैं। कर्म स्वयं की खोज है। और जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है, वही केवल स्वतंत्रता भी पा जाता है। स्वतंत्रता हो भी तो तभी सकती है जब स्व का अनुभव हो। स्वयं का होना ही जब ज्ञात नहीं है तब तक
8V 

9 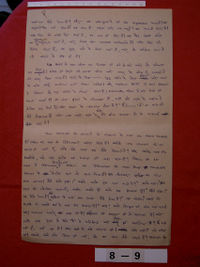
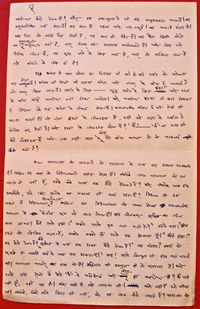
Naye Sanket (नये संकेत), notes 219 - 221 - स्वतंत्रता कैसे संभव है? और उस स्वानुभव से एक अनुशासन आता है। वह बाह्यारोपित नहीं होता है। वह होता है सहज और स्वस्फूर्त। वह आता है अंतर से। और फिर जो नीति पैदा होती है, वह बात ही और है। वह फिर किसी ढांचे का सायास अनुकरण नहीं है, वरन अंतस की अप्रयास अभिव्यक्ति है। और फिर जो नैतिक जीवन है, वह कुछ पाने के लिए नहीं है, वरन जो पा लिया गया है उसे बांटने के लिए ही है।
- १७. आंख में पड़ा छोटा सा तिनका भी बड़े से बड़े पर्वत को ओझल कर लेता है। आंख की छोटी सी पलक आंख और जगत के बीच में आ जमी है तो जगत छिप जाता है। दर्शन के लिए- शुद्ध दर्शन के लिए द्रष्टा और द्दश्य के बीच कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। और अवरोध उतना ही बड़ा हो जाता है जितना कि वह आंख के निकट होता है। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसी ही घटना घटती है। जो चीज द्रष्टा के निकटतम है, वही उसे सत्य के दर्शन से वंचित कर देती है। और द्रष्टा के निकटतम कौन है? ’ ‘मैं- ‘मैं’ का भाव ही मेरे निकटतम है और तब वही सत्य के और मेरे बीच बाधा हो तो आश्चर्य क्या है?
- १८. परमात्मा को जानना है तो परमात्मा के साथ एक हो जाना आवश्यक है। लेकिन यह बात तो विरोधाभासी प्रतीत होती है। क्योंकि जिस परमात्मा को हम जानते ही नहीं हैं, उसके साथ एक कैसे हो सकते हैं? और जिसके साथ एक हो जाएंगे, उसे फिर जानने का सवाल ही कहां उठता है? निश्चय ही इस कथन में विरोधाभास दिखाई पड़ता है, लेकिन इस विरोधाभास को समझ लेना आध्यात्मिक साधना के ठीक सूत्र को जान लेना है। एक चित्रकार सूर्यास्त का चित्र बना रहा था। मैंने उससे पूछाः ‘सबसे पहले तुम क्या करते हो? ’ उसने कहाः ‘जिस द्दश्य को चित्रित करना है, सबसे पहले मैं उसमें एक हो जाता हूं।’ मैंने पूछाः ‘यह कैसे संभव है? जैसे सूर्यास्त के साथ एक होना कैसे संभव है? ’ वह बोलाः ‘स्वयं को भूलते ही व्यक्ति सर्व के साथ एक हो जाता है।’ आह! उसने बिल्कुल ही ठीक बात कह दी थी। परमात्मा अर्थात वह सब जो है। अस्तित्व की समग्रता ही तो परमात्मा है। और उससे एक होने में मेरे ‘मैं’ के अतिरिक्त और कौन सा अवरोध है? मैं जहां नहीं हूं, वहीं वह है। और यही है उसे जानना भी। और यही है उसे जीना भी। क्योंकि, जिसे हमने जीआ ही नहीं, उसे हम जान कैसे सकते हैं? परमात्मा को
10 
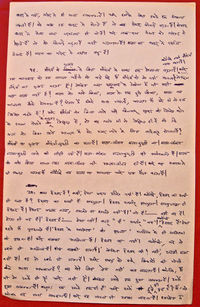
Naye Sanket (नये संकेत), notes 221 - 223 - बाहर से नहीं, भीतर से ही जाना जा सकता है। और इसके लिए उसमें एक हो जाना जरूरी है। उसे जब हम बाहर से देखते हैं तो संसार दिखाई पड़ता है। संसार बाहर से देखा गया परमात्मा ही तो है। और जब हम संसार को भीतर से देखते हैं तो जो दिखाई पड़ता है वही परमात्मा है। सत्य का बाहर से दर्शन संसार है। सत्य का भीतर से दर्शन प्रभु है।
- १९. सौंदर्य के सृजन के लिए सौंदर्य के साथ एक हो जाना पड़ता है। क्योंकि तभी सौंदर्य जाना जाता है। और उस कलाकार को हम पागल कहेंगे जो कहे कि मैं सौंदर्य को तो नहीं जानता हूं लेकिन सौंदर्य का सृजन करता हूं! लेकिन क्या सदाचार के संबंध में भी यही बात सत्य नहीं है? सत्य को जाने बिना, सत्य से एक हुए बिना, सत्य का आचरण कैसे हो सकता है? चेतना में जिसे जाना जाता है, आचरण कैसे हो सकता है? चेतना में जिसे जाना जाता है, आचरण में उसे ही तो हम चित्रित करते हैं? और सौंदर्य को बिना जाने यदि चित्रकार सुंदर को चित्रित करने के स्वप्न देखने के कारण विक्षिप्त है, तो वह व्यक्ति भी तो विक्षिप्त ही है जो कि सत्य को बिना जाने आचरण में उसे उतार लाने के लिए कटिबद्ध हो गया है? सौंदर्य का सृजन सौंदर्यनुभूति का फल है। सत्य-जीवन सत्यानुभूति का। सत्य-जीवन सत्यानुभूति पाने की सीढ़ी नहीं है। सत्य-जीवन सत्यानुभूति की अभिव्यक्ति है। सत्य को पाए बिना साधा गया सत्य जीवन की असत्य जीवन ही है। और वह असत्य से भी ज्यादा घातक है क्योंकि वह सत्य का आभास और भ्रम पैदा करता है।
- २०. क्या ईश्वर है? नहीं, ऐसा प्रश्न उचित नहीं है। क्योंकि, ईश्वर का अर्थ ही क्या है? ईश्वर का अर्थ है समग्रता। ईश्वर अर्थात समग्रता। समग्र सत्ता ही ईश्वर है। ईश्वर प्रथक तत्व, व्यक्ति या शक्ति नहीं है। ‘जो है’- वही वह है। होना ही वह है। ‘ईश्वर है’- ऐसा नहीं। वरन ‘है’ अर्थात ‘वह’। क्योंकि ‘ईश्वर है’ ऐसा कहने में पुनरुक्ति है। ‘ईश्वर के अस्तित्व’ को पूछना अस्तित्व के ही अस्तित्व को पूछना है। और सबका अस्तित्व है। शेष सबकी सत्ता है। लेकिन ईश्वर की? नहीं, उसकी सत्ता नहीं है। वह तो स्वयं ही सत्ता है। और समग्र को और की भांति कैसे जाना जा सकता है? वह मेरे लिए ज्ञेय नहीं बन सकता है। क्योंकि, मैं भी तो उसमें ही हूं और वही हूं। लेकिन उससे एक हुआ जा सकता है। उसमें डूबा जा सकता है। वस्तुतः हम उससे एक ही हैं और उसमें डूबे ही हुए हैं।’ ‘मैं’ को खोकर यह जान जा सकता है। और यह जानना ही उसका जानना है। इसलिए मैं
11 

Naye Sanket (नये संकेत), note 223 - कहता हूं कि प्रेम ही उसका ज्ञान है। प्रेम में ही वह जान जाता है क्योंकि प्रेम में ‘मैं’ मिट जाता है। ‘मैं’ जहां है, वहां वह नहीं है। ‘मैं’ जहां नहीं है, वहीं वह है। सुना है कि एक नमक की पुतली सागर को जानने गई थी। उसने सागर को जान लिया लेकिन फिर वह लौटी नहीं, क्योंकि सागर जानने में ही वह सागर हो गई थी। सागर को जानने का सागर होने के अतिरिक्त उसके पास और उपाय ही क्या था? परमात्मा को जानने का भी मनुष्य के पास परमात्मा होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
12 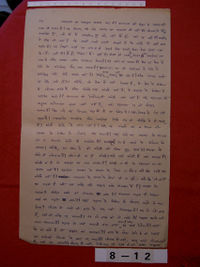
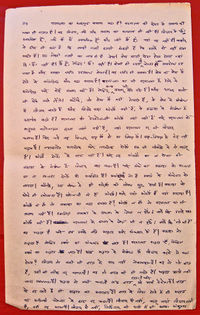
Naye Sanket (नये संकेत), note 224 - २१. परमात्मा का अकाट्य प्रमाण क्या है? परमात्मा की दिशा में प्रमाण की भाषा ही गलत है। वह विचार, तर्क और प्रमाण का आयाम ही नहीं है। विचार में ‘मैं’ उपस्थित हूं, तर्क में मैं उपस्थित हूं और जहां मैं हूं, वहां वह नहीं है। कबीर ने ठीक ही कहा है कि उसकी गली इतनी संकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते हैं। उस संकरी गली का नाम ही है प्रेम। प्रेम यानी मेरा ऐसा होन जहां कि ‘मैं’ नहीं है। मैं हूं, लेकिन ‘मैं’ नहीं है। ऐसी ही दशा में चेतना से अवरोध हट जाता है और उसका दर्शन उपलब्ध होता है। वह दर्शन ही प्रमाण है। प्रेम का प्रेम में होने के अतिरिक्त और क्या प्रमाण है? परमात्मा का भी परमात्मा में होने के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अन्य प्रमाण भी दिए गए हैं। और शायद आगे भी दिए जाते रहेंगे। क्योंकि, जो प्रेम में नहीं हो पाते हैं, वे प्रेम के संबंध में विचार करते हैं और जिनके पास आंखें नहीं हैं, वे प्रकाश के संबंध में विचार करते हैं। परमात्मा को देखने वाली आंखें जहां नहीं हैं और परमात्मा को अनुभव करने वाला हृदय जहां नहीं है, वहां परमात्मा पर भी विचार चलता है। फिर चाहे वह विचार पक्ष में हो या विपक्ष में। पक्ष-विपक्ष से भेद नहीं पड़ता है। तथाकथित आस्तिक और नास्तिक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आंखें दोनों के पास नहीं हैं? और यह आंखों का न होना ही प्रकाश के संबंध में विवाद बन जाता है। और अंधे का प्रकाश को मानना या न मानना दोनों ही अर्थहीन हैं। अर्थपूर्ण तो है स्वयं के अंधेपन को जानना। क्योंकि, उस बोध से ही आंखों की खोज शुरू होती है। प्रकाश को थोड़े ही खोजना है। खोजना तो हैं आंखें। और जहां आंखें हैं वहां प्रकाश है, आंखें न हों तो प्रकाश का क्या प्रमाण है? आंखें न हों तो परमात्मा का भी प्रमाण नहीं है। इसलिए प्रकाश के प्रमाण के लिए न पूछेः जानें कि हमारे पास आंखें नहीं हैं। परमात्मा के प्रमाण के लिए भी न पूछेः जानें कि ‘जो भी है’ वह अज्ञात है और हम उसके प्रति अज्ञान और अंधकार में हैं। प्रकाश तो अज्ञात है लेकिन स्वयं का अंधापन ज्ञात है। परमात्मा अज्ञात है, लेकिन स्वयं का अज्ञान ज्ञात है। परमात्मा अज्ञात है, लेकिन स्वयं का अज्ञान ज्ञात है। अबग अज्ञात के संबंध में विचार करने से क्या होगा? वह तो जो ज्ञात के पार नहीं ले जा सकता है। वह तो जो ज्ञात है, उसी की लीक पर चलता है। वह तो ज्ञात की ही गति है। अज्ञात उससे नहीं जाना जा सकता है। वह तो जो ज्ञात है, उसी की लीक पर चलता है। वह तो ज्ञात की ही गति है। अज्ञात उससे नहीं जाना जात सकता है। अज्ञात तो तभी आता है जब ज्ञात हटता है और उसे मार्ग दे देता है। ज्ञात के हट जाने में ही अज्ञात का आगमन है। ज्ञात के विदा होने में ही अज्ञात का अतिथि चेतना के द्वार पर आता है। विचार में नहीं, वरन जहां विचार नहीं है, वहीं वह आता है। विचार में नहीं, निर्विचार की भूमि में ही उसका अंकुरण
13 
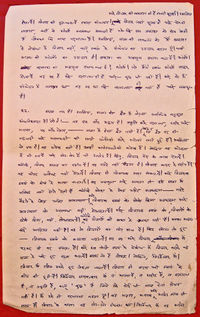
Naye Sanket (नये संकेत), notes 224 - 225 - होता है। विचार की मृतधारा है हमारा अंधापन। और विचार की व्यस्ता ही है हमारी मूर्च्छा। इसलिए विचार जहां शून्य है और चेतना सजग, वहीं वे आंखें उपलब्ध हो जाती हैं जो कि उस प्रकाश को देख लेती हैं जिसका कि नाम परमात्मा है? इसलिए सत्य की साधना को मैं प्रकाश के संबंध में विचार नहीं, वरन स्वयं के अंधेपन का उपचार कहता हूं। धर्म आत्मा की आंखों का उपचार है। प्रकाश का अकाट्य प्रमाण क्या है? आंखें। परमात्मा का अकाट्य प्रमाण क्या है? आंखें। जो मैंने स्वयं आंखें पाकर देखा वह यह है कि परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। और जो मैं अंधेपन में जानता था वह यह था कि परमात्मा ही नहीं है और सब कुछ है।
- २२. सत्य एक है। इसलिए, सत्ता को द्वैत में तोड़ना सर्वाधिक बद्धमूल अंधविश्वास है। ‘जो है’- वह एक और अद्वैत है। प्रकृति और परमात्मा, शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन- सत्ता में ऐसा द्वैत नहीं है। लेकिन इस द्वैत पर ही जड़वादी और आत्मवादी की सारी भ्रांतियां और अतियां खड़ी हुई हैं। अस्तित्व तो एक है। वह अनेक नहीं है। उसकी अभिव्यक्तियां अनेक हैं। लेकिन वह अनेकता में भी एक है और खंड-खंड में भी अखंड है। किंतु, विचार भेद को जन्म देता है। क्योंकि, विचार सतह का दर्शन है। वह गहरे नहीं पैठता है। विचार बाहर से दर्शन है। वह भीतर प्रविष्ट नहीं होता है। विचार से विचारक खड़ा हो जाता है। और विचारक स्वयं को शेष से अन्य जानता है। यह पृथकता और अन्यता ही उसे सत्ता में प्रविष्ट नहीं होने देता है। क्योंकि प्रवेश के लिए चाहिए अपृथकता- गहरे पैठने के लिए चाहिए अनन्यता और विचारक स्वयं को खोए बिना अपृथकता और अनन्यता को उपलब्ध नहीं हो सकता है। और विचारक स्वयं को, विचारों को खोए बिना, नहीं खो सकता है। क्योंकि वह विचारों की छाया से ज्यादा नहीं है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह तो विचारों को जोड़ मात्र है। फिर खोना तो दूर- विचारक स्वयं को बचाना चाहता है। यह वह और विचार में पड़ कर ही कर सकता है। और इस भांति सत्य के संबंध में विचार करके वह सत्य से और दूर पड़ता जाता है। सत्य तो है निकट। लेकिन, निर्विचार में। विचार में चित्त उससे दूर निकल जाता है। विचार हो सत्य और स्वयं के बीच वकी दूरी है। निर्विचार साक्षात्कार में न आत्मा है, न शरीर है, न परमात्मा है, न प्रकृति है, वरन ‘कुछ’ है जिसे कि कोई भी नाम देना संभव नहीं है। मैं उसे ही परमात्मा कहता हूं। वह अज्ञात, अनाम और अखंड तत्व ही सत्य है। विचार के कारण वह खंड-खंड दिखता था। निर्विचार में वह अखंड
14 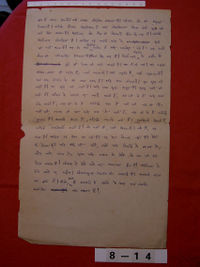
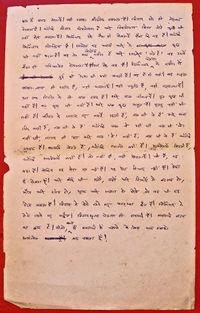
Naye Sanket (नये संकेत), note 225 - रूप से प्रकट होता है। वही उसका मौलिक स्वरूप है। विचार उसे ही तोड़ कर देखता है। क्योंकि चिचार विश्लेषण है और विश्लेषण बिना तोड़े कुछ भी नहीं देख सकता है। निर्विचार उसे वैसा ही देखता है जैसा कि वह है। क्योंकि निर्विचार निष्क्रिय है। इसलिए वह अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता है। वह तो बस निर्दोष दर्पण है और इसलिए ‘जो है’ वह उसमें वैसा ही प्रतिफलित हो जाता है जैसा कि वह है। निर्विचार चेतना के दर्पण में दुई की रेखा भी नहीं बनती है। वह है ही नहीं। वह अज्ञात जीवन तत्व ही शरीर है, वही आत्मा है। वही प्रकृति है, वही परमात्मा है। उस एक संगीत के ही सब स्वर हैं। और सब जीवन है। मृत कुछ भी नहीं है। जड़ कुछ भी नहीं है। और सब कुछ अमृत है। मृत्यु कहीं भी नहीं है। जीवन के सागर पर लहरें उठती हैं, तब भी वे हैं और जब गिर जाती हैं, तब भी वे हैं क्योंकि जब वे उठीं थी तब भी ‘वे’ नहीं थी, सागर ही था और जब ‘वे’ नहीं है, तब भी वे हैं क्योंकि सागर है। व्यक्ति मिटते हैं, क्योंकि व्यक्ति नहीं हैं। आस्तिकताएं मिटती हैं, क्योंकि आस्तिकताएं नहीं हैं। जो नहीं है, वही मिटता है। जो है, वह सदा है। लेकिन यह मेरा मत नहीं है। यह मेरा विचार नहीं है। ऐसा मैं देखता हूं। और कोई भी मतों, पक्षों और विचारों से तटस्थ हो, मौन और शांत हो, शून्य और सजग हो देखें तो वह भी देख सकता है। विचार से देखे जाने पर जगत सत्ता द्वैत है। निर्विचार से देखे जाने पर अद्वैत। विचार-शून्य चेतना ही समाधि है। समाधि सत्य का द्वार है। मित्रो, क्या मैं समाधि में चलने के लिए आप सबको आमंत्रित कर सकता हूं?
