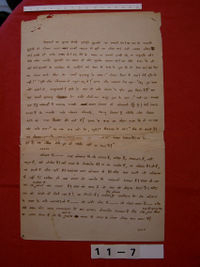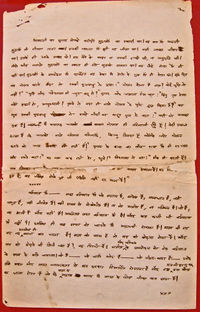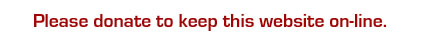Manuscripts ~ Punruddhar (पुनरुद्धार): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dhyanantar (talk | contribs) No edit summary |
Dhyanantar (talk | contribs) (add transcripts) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
;notes | ;notes | ||
:7 sheets. One sheet repaired. | :7 sheets. One sheet repaired. | ||
:Published as ch.28, 29 and 31 of ''[[Prem Ke Swar (प्रेम के स्वर)]]''. | |||
; see also | ; see also | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
:{| class = "wikitable" | :{| class = "wikitable" | ||
|- | |- | ||
!| ''' | !| '''sheet no''' || '''original photo''' || '''enhanced photo''' || '''Hindi transcript''' | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 1 || [[image:man0932.jpg|200px]] || [[image:man0932-2.jpg|200px]] || | | 1 || [[image:man0932.jpg|200px]] || [[image:man0932-2.jpg|200px]] || rowspan = "3" | ''[[Prem Ke Swar (प्रेम के स्वर)]]'', chapter 28 | ||
:मैं देखता हूं कि मनुष्य का मन अतियों में जीता है। घड़ी के पेंडुलम की भांति ही उसकी गति है। वह मध्य में कभी नहीं ठहरता। एक ‘अति’ से दूसरी ‘अति’--यही उसका यात्रा-पथ है, और अति, दुख की जननी है। अति, चिंता और तनाव पैदा करती है। अति स्वयं से बाहर जाना है, क्योंकि अति, साम्य को, समता को खोना है। स्वयं में ठहरने की भूमिका समता है। स्वयं में होना समता में हुए बिना संभव नहीं। समता अंतर्गमन का द्वार है। अति बहिर्गमन का। अति ही विषमता है। समता स्वास्थ्य है। विषमता अस्वास्थ्य। किंतु मनुष्य चित्त अस्वस्थ ही रहना चाहता है क्योंकि अस्वास्थ्य में ही उसका जीवन है, स्वास्थ्य की दिशा में गति तो उसकी मृत्यु को ही आमंत्रण है। इसलिए एक अति से ऊब जाता है, तो वह तत्क्षण दूसरी अति के प्रति आकर्षित हो जाता है। विराम का अवसर वह नहीं देता। अंतराल को क्षण भर भी रिक्त छोड़ने की भूल वह नहीं करता। रिक्तता उसके लिए संधातक है। तनाव की स्थिति सदा ही बनी रहे यही उसके लिए शुभ है। वह सदा दौड़ता रहे, दौड़ता ही रहे, यही उसके लिए प्राणदायी है। क्योंकि ठहरते ही, रुकते ही उसके दर्शन होते हैं जो कि आत्मा है। और आत्मा को पाने पर चित्त वैसे ही नहीं पाया जाता है, जैसे कि सूर्योदय होने पर रात्रि नहीं पाई जाती। | |||
:रात्रि कुछ संन्यासियों के बीच था। उन्हें देखता था। उनके चित्त को देखता था। उनकी क्रियाओं को देखता था। वे सब कभी गृहस्थ थे। उस जीवन के विरोध और प्रतिक्रिया में अब वे संन्यासी हैं। उस जीवन को अब उन्होंने सब भांति उलटा कर लिया है। चित्त वही है, लेकिन दिशा विरोधी है। भोग छोड़ा तो त्याग को पकड़ लिया। धन छोड़ा तो दरिद्रता को पकड़ लिया। तब संसार की खोज में जाते थे, अब संसार से भागे जा रहे हैं। अति बदल गई है, किंतु अति फिर भी वहीं की वहीं है। | |||
:एक मित्र हैं। वे कहते हैंः ‘स्त्री नरक का द्वार है।’ यह भी मैं जानता हूं कि कभी वे मानते थे कि स्त्री के अतिरिक्त और कोई स्वर्ग नहीं है। पहले वे स्त्री के लिए लड़ते थे, अब स्त्री से लड़ते हैं। किंतु उनके चित्त का केंद्र आज भी स्त्री बनी हुई है। काम (सेक्स)की ओर जावें या काम के विरोध में, दोनों ही स्थितियों में चित्त काम वासना पर ही घूमता रहता है। काम के विरोध में काम से मुक्ति नहीं है। जो स्त्री को स्वर्ग मानता है, वह तो कामुक है ही, जो उसे नरक मानता है वह भी कामुक ही है। | |||
:शरीर के भोग में ही जाने वाले व्यक्ति हैं, और शरीर को पीड़ा देकर आनंद अनुभव करने वाले व्यक्ति भी हैं। किंतु स्मरण रहे कि दोनों ही देहवादी हैं। शरीर भोग ही उलटा होकर शरीर-योग बन जाता है। इंद्रिया-भोग ही इंद्रिय-दमन बन जाता है। चेतना दोनों ही अतियों में शरीर के तट से बंधी रहती है। इस भांति आत्मा की यात्रा न कभी हुई है, और न कभी हो ही सकती है। | |||
:राग से विराग की अति पर चले जाना ज्ञान नहीं है। | |||
:सुख से दुख की अति पर चले जाना संन्यास नहीं है। | |||
:सत्य द्वंद्व में और अतियों के चुनाव में नहीं, वरन संयम में और समता में है। | |||
:जीवन का रहस्य और उसे खोलने की कुंजी संयम है; संयम यानी चित्त की अतियों से मुक्ति। अतियों से मुक्त होना, चित्त से ही मुक्त हो जाना है। | |||
:एक धनपति युवक थाः श्रोण। वह अपूर्व रूप, से सुंदर था। उसके वीरबहूटी से लाल तथा नवनीत से कोमल तलवे थे। उसके उन सुंदर तलवों पर मुलायम बाल भी उगे हुए थे। सम्राट बिंबिसार तक को उसे और उसके तलवों को देखने का कुतूहल हुआ था। श्रोण का जीवन वैभव-भोग में ही बीतता था। सुख ही सुख के सागर में वह तैरता था। किंतु फिर भी उसका चित्त शांत न था। आंनद के लिए वह भी लालायित था। जीवन अर्थ के ओर-छोर की खोज उसके मन को भी पीड़ित करती थी। धीरे-धीरे उसका चित्त सुखों से भी ऊब गया। सुख की संवेदनाएं भी बोथली हो गईं। धन, वैभव और भोग सब नीरस हो आया। ऊब की इसी चित्त-दशा में उसने बुद्ध के दर्शन किए और उनकी वाणी सुनी। उसके हृदय में नई अनुभूतियों की आशा जगी। वह विरक्त हो गया और उसने तप का मार्ग अपना लिया। चित्त ने भोग की प्रतिक्रिया में, विरोध में, दमन की दिशा सुझाई। वह भांति-भांति से शरीर को कष्ट देने लगा। मन बहुत अदभुत है। वही भोग की नई-नई विधियां | |||
:खोजता है। वही शरीर-दमन और उत्पीड़न के नये-नये आविष्कार करता है। कामसूत्र भी वही रचता है, आत्म-हिंसक तपश्चर्या के मार्ग भी वही खोजता है। अतियों की खोज के लिए वह सदा ही अति-उत्सुक है। श्रोण भी आत्म-उत्पीड़न में लग गया। शरीर के घोर दमन में वह रस लेने लगा। भिक्षु साफ-सुथरे मार्गों पर चलते तो वह कुश-कंटकों से भरी भूमि पर ही चलता। शीत-ताप में शरीर को सताता। भूख-प्यास में शरीर को सताता। उसकी सुंदर देह सूख कर काली पड़ गई। उसके कोमल तलवों में घाव बन गए और रक्त बहने लगा। उसका शरीर अशक्त और रुग्ण हो गया। वह तपस्वी जो हो गया था! | |||
:एक दिन बुद्ध तथाकथित तपस्वी श्रोण के पास गए। उसकी दशा देख उन्हें दया आनी स्वाभाविक ही थी। उन्होंने उससे बहुत प्रेम से पूछाः श्रोण! तूने कभी वीणा बजाई है? श्रोण को स्मरण आया। वह तो वीणा बजाने में बहुत कुशल था। उसने कहाः हां, भंते! तब बुद्ध ने पूछाः क्या तार बहुत ढीले हों तेा उनसे संगीत पैदा होता है? श्रोण बोलाः नहीं भंते! और यदि तार बहुत कसे हों तो? श्रोण ने कहाः तब भी नहीं, भंते! फिर संगीत कब पैदा होता है? यह सुन श्रोण जैसे निद्रा से जाग गया। उसकी आंखों से एक नशा विलीन हो गया। वह बोलाः भंते, वीणा के तारों से संगीत का जन्म तभी होता है, जब वे न तो अति ढीले हों और न अति कसे हों। उस सूक्ष्म संतुलन में ही संगीत पैदा होता है। बुद्ध ने कहाः फिर श्रोण, स्मरण रख कि जीवन के संगीत का भी नियम यही है। | |||
:जीवन संगीत में हो, तो ही सत्य की अनुभूति होती है। | |||
:समता, संतुलन, और संयम से संगीत पैदा होता है। चित्त अतियों में होता है तो विसंगति में होता है। वह जैसे ही अतियों के, द्वंद्वों के मध्य में ठहरता है, वैसे ही संगीत को पा लेता है। इस संगीत में आना ही स्वयं में आना है वही स्वास्थ्य है। वही सत्य है। वही धर्म है। | |||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 2 || [[image:man0933.jpg|200px]] || [[image:man0933-2.jpg|200px]] | | 2 || [[image:man0933.jpg|200px]] || [[image:man0933-2.jpg|200px]] | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 3 || [[image:man0934.jpg|200px]] || [[image:man0934-2.jpg|200px]] | | 3 || [[image:man0934.jpg|200px]] || [[image:man0934-2.jpg|200px]] | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 4 || [[image:man0935.jpg|200px]] || [[image:man0935-2.jpg|200px]] || | | 4 || [[image:man0935.jpg|200px]] || [[image:man0935-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Prem Ke Swar (प्रेम के स्वर)]]'', chapter 29 | ||
:एक मंदिर के द्वार से निकल रहा था। देखा, सैकड़ों व्यक्ति भीतर आ-जा रहे हैं। मैं भी एक कोने में रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। परमात्मा को छोड़ कर वे और सारी बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में न तो प्रेम था, न प्रार्थना थी। फिर वे क्यों मंदिर में जा रहे थे? वे किसे धोखा दे रहे थे? क्या संसार को और स्वयं को धोखा देते देते उन्होंने परमात्मा को भी धोखा देने का साहस कर डाला था? | |||
:स्मरण करता हूं तो बहुत-से मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों की याद मुझे आती है। उनमें जाने वालों के चेहरे भी मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। लेकिन फिर बहुत आश्चर्य होता है। जीवन भर प्रभु के मंदिरों की यात्रा करने वालों में से कितने उसके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं? क्या इन मंदिरों से उसका मंदिर बहुत बहुत दूर नहीं है? | |||
:मनुष्य का हृदय ही जब तक परमात्मा का मंदिर न बने, तब तक किसी भी मंदिर में उसका प्रवेश नहीं हो सकता है। | |||
:प्रेम ही जब तक प्रार्थना न बने तब तक कोई प्रार्थना प्रार्थना नहीं हो सकती है। | |||
:सत्य की जब तक स्वयं ही अनुभूति न हो तब तक शास्त्र क्या करेंगे? शब्द क्या करेंगे? सिद्धांत क्या करेंगे? | |||
:संसार भर में खोजने पर अंत में ज्ञात होता है कि वह तो स्वयं में ही है। | |||
:सत्य स्वयं में है। धर्म स्वयं में है। जो उसे स्वयं में नही खोजता है, वह व्यर्थ खोजता है, | |||
उसकी सब खोज मिथ्या है। उसका धर्म, उसके शास्त्र, उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा, उसका परमात्मा सब झूठे हैं। | |||
:वह परमात्मा के मंदिरों में नहीं, अपनी ही वासना के घरों में आता-जाता है। वह प्रार्थना के मौन में नहीं, अपनी ही आकांक्षाओं के शब्द-जाल में भटकता है। उसकी आंखें उसके स्वार्थ के क्षितिज से कभी ऊपर नहीं उठतीं और उसके हृदय में परमात्मा की नहीं, उसकी अपनी अहंता की ही मूर्ति सदा प्रतिष्ठित रहती है। | |||
:एक गांव में नानक का आगमन हुआ था। वे तो धर्म की बात करते थे, हिंदू और मुसलमान की नहीं। उनका तो परमात्मा से वास्ता था, मस्जिद और मंदिर से नहीं। उस गांव के नवाब ने उससे कहाः आपके लिए तो मस्जिद और मंदिर बराबर | |||
:है, तो क्या आप आज मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को तैयार हैं? नानक ने बहुत आनंदित होकर कहाः जरूर, जरूर! परमात्मा की प्रार्थना में सम्मिलित होने से बड़ा आनंद और क्या है? फिर, नवाब, काजी और गांव के बहुत-से लोग मस्जिद गए। सभी नानक की नमाज देखना चाहते थे। मस्जिद में पहुंच कर काजी और नवाब और उनके साथी नमाज अदा करने लगे किंतु नानक एक कोने में खड़े ही गए और चुपचाप उनकी ओर देखने लगे। उनको इस भांति खड़ा देख कर नवाब और काजी को बहुत क्रोध आने लगा। वे बीच बीच में नानक की ओर क्रोध से देख भी लेते थे। फिर किसी भांति जल्दी-जल्दी उन्होंने नमाज पूरी की और सब नानक पर टूट पड़े। वे नानक को धोखेबाज और वचन तोड़ने वाला कहने लगे। नवाब ने क्रोध से आंखें लाल करके नानक को डांटा और कहाः आपने नमाज क्यों नहीं की? आप नमाज में सम्मिलित क्यों नहीं हुए? नानक यह सब देख खूब हंसने लगे और बोलेः मैं तो नमाज में सम्मिलित होने आया था, लेकिन जब आपने ही नमाज नहीं पढ़ी तो मैं चुपचाप दूर खड़ा आपके खेल को देखता रहा। और करता भी क्या? आप सबका ध्यान तो मेरी ओर था। परमात्मा की ओर तो किसी का भी ध्यान नहीं था। यह कैसी इबादत? यह कैसी प्रार्थना? परमात्मा के निकट इस भांति कैसे हुआ जा सकता है? | |||
:मैं भी मंदिरों के, मस्जिदों के, गिरजों के कोनों में खड़े होकर देखता रहा हूं। और जो देखा, उससे ज्यादा असत्य मनुष्य के जीवन में और कुछ भी नहीं पाया। जब धर्म ही असत्य हो तो शेष सब अपने-आप ही असत्य हो जाता है। मनुष्य का सब कुछ असत्य हो गया है क्योंकि उसका परमात्मा असत्य है, उसकी प्रार्थना असत्य है। परमात्मा जीवन का आधार है और केंद्र है, और यदि वही असत्य है तो फिर और क्या सत्य हो सकता है? | |||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 5 || [[image:man0936.jpg|200px]] || [[image:man0936-2.jpg|200px]] | | 5 || [[image:man0936.jpg|200px]] || [[image:man0936-2.jpg|200px]] | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 6 || [[image:man0937.jpg|200px]] || [[image:man0937-2.jpg|200px]] || | | 6 || [[image:man0937.jpg|200px]] || [[image:man0937-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Prem Ke Swar (प्रेम के स्वर)]]'', chapter 31 | ||
:आकाश में वर्षा के पहले बादल घिरे हैं। ग्रीष्म में प्यासी हो उठी पृथ्वी के प्राण आनंद से पुलकित हो रहे हैं। पक्षी मंगल-गीत गा रहे हैं और वृक्षों की आंखें प्रेम और प्रतीक्षा से बादलों को निहार रही हैं। एक पुराने बड़-वृक्ष के नीचे मैं भी इस आनंदोत्सव में सम्मिलित हुआ बैठा हूं। निकट ही जनपथ है। उसपर से लोग आ-जा रहे हैं। मैं उन्हे देखता हूं। वे अपने में घिरे हैं। न उन्हें ऊपर घिरे बादलों का पता है, न नीचे हो रहे इस विराट स्वागत-समारोह का। पक्षियों के गीत उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहे और न पृथ्वी की प्रार्थनाएं। वे अपने में बंद हैं। वर्तमान में वे नहीं हैं। अतीत, मृत अतीत में ही उनका मन यात्रा किए जाता है। मन अतीत ही है। वह भी मृत है उसका मुख सदा ही वर्तमान से विमुख है। वह वर्तमान में कभी होता ही नहीं। उसे वर्तमान की सतत जीवंत और अपरिचित घड़ियां नहीं, वरन अतीत की परिचित और जड़ परिस्थितियां ही प्रिय हैं। जीवन में तो वे परिस्थितियां अब नहीं, इसलिए स्मृति में, मन-स्थितियों की भांति ही वह उन्हें जिये जाता है। जीवन नित-नूतन है, किंतु मन सदैव ही पुरातन बना रहता है। | |||
:एक राजा के महल में मैं गया था। उस महल के तलघरे में न मालूम किस किस सदी का कूड़ा-कबाड़ इकट्ठा था। ऐसा ही मनुष्य का मन है। उसमें भी अतीत की धूल इकट्ठी होती रहती है। यह धूल चेतना के दर्पण को इस भांति ढंक लेती है कि फिर उसमें जीवन के प्रतिफलन बनने बंद ही हो जाते हैं। अतीत बोझ हो जाता है। अतीत बंधन हो जाता है। अतीत एक ऐसा जादुई घेरा हो जाता है कि उसका अतिक्रमण असंभव प्रतीत होता है। चेतना की अमुक्ति यही है। आत्मा के लिए जड़ता यही है। मन के, मृत मन के अतिरिक्त आत्मा पर और कोई बंधन कहां हैं? | |||
:जीवन के अनुभव के लिए मन की कारा से मुक्ति आवश्यक है। | |||
:मन की कारा से मुक्त जीवन को ही मैं परमात्मा की अनुभूति जानता हूं। | |||
:जीवन और मन की दिशाएं विपरीत हैं। मन मृत्यु की ओर बहता है। वह मृत ही है। मन सदा बासा है। उसका जीवंत से संपर्क ही नहीं होता है। प्रकाश से जैसे अंधेरा दूर-दूर रहता है, ऐसे ही वह भी जीवन से दूर-दूर रहा आता है। | |||
:श्रावस्ती का मृगार श्रेष्ठ करोड़ों मुद्राओं का स्वामी था। वह मन में अपनी मुद्राएं ही गिनता रहता। उनकी गणना में ही वह जीता था। वही उसका जीवन था। उनमें ही उसके प्राण थे। उस घेरे के बाहर न उसकी दृष्टि थी, न अनुभूति थी। सोते और जागते मुद्राओं का स्वप्न ही उसे सुलाए रखता था। वह जैसे होश में ही नहीं था। मुद्राओं के सम्मोहन में मूर्च्छित वह होश में होने के भ्रम में ही होता था। एक दिन वह भोजन करने बैठा तो उसकी पुत्रवधु ने पूछाः भोजन कैसा है, तात? कोई त्रुटि तो नहीं? त्रुटि और विशाखा सी चतुर बहू से? मृगार कौर चबाता हंस पड़ाः किंतु तुम ऐसा क्यों पूछती हो, आयुष्मती? तुमने तो सदा ही ताजे भोजन से मुझे तृप्त किया है? यह सुन उसकी पुत्रवधु ने दृष्टि नीची कर बहुत दुख से कहाः यही तो आपका भ्रम है। मैं आज तक आपको बासा भोजन ही खिलाती रही हूं। मेरी प्रबल इच्छा है कि आपको ताजे व्यंजन खिलाऊं, किंतु विवश हूं, क्योंकि ताजे भोजन करने को आप तैयार ही नहीं हैं! मृगार के हाथ का कौर हाथ में ही रह गया और उसने कहाः यह क्या कह रही हो शुभे। विशाखा ने कहाः ठीक ही कहती हूं। मन जिसका बासा है, उसका सब-कुछ, सारा जीवन ही बासा हो जाता है। मन जिसका मृत है, वह जीवित होते हुए भी जीवित नहीं रह जाता है। | |||
:वर्तमान में, सदा वर्तमान में जो सजग है, सचेत है, सावधान है, वही जाग्रत है, वही जीवित है। वही सत्ता से संबंधित है। न तो अतीत है, न भविष्य है। जो है, वह अभी है और यहीं है। अस्तित्व सदा वर्तमान में है। मन कभी भी वर्तमान में नहीं है। इसीलिए मन सत्ता को जानने में असमर्थ हो जाता है। सत्य की राह पर वह इसीलिए बाधा बन जाता है। सत्य को पाना है तो मन को छोड़ना होता है। मन को छोड़ने की विधि क्या है? वह विधि हैः अतीत और भविष्य के सम्मोहन को तोड़ कर वर्तमान के सत्य के प्रति जागना जो है, जो चारों ओर है, जो भीतर-बाहर है, उसके प्रति सहज और सतत जागरूकता से मन क्रमशः विसर्जित हो जाता है, और तब मन की मृत्यु पर उस मौन का जन्म होता है जो कि सत्य के अज्ञात सागर में यात्रा के लिए नौका बन जाता है। | |||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 7 || [[image:man0938.jpg|200px]] || [[image:man0938-2.jpg|200px]] | | 7 || [[image:man0938.jpg|200px]] || [[image:man0938-2.jpg|200px]] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:34, 3 February 2019
Reorientation of Self
- year
- 1967
- notes
- 7 sheets. One sheet repaired.
- Published as ch.28, 29 and 31 of Prem Ke Swar (प्रेम के स्वर).
- see also
- Osho's Manuscripts
sheet no original photo enhanced photo Hindi transcript 1 
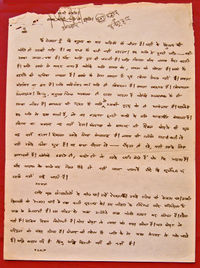
Prem Ke Swar (प्रेम के स्वर), chapter 28 - मैं देखता हूं कि मनुष्य का मन अतियों में जीता है। घड़ी के पेंडुलम की भांति ही उसकी गति है। वह मध्य में कभी नहीं ठहरता। एक ‘अति’ से दूसरी ‘अति’--यही उसका यात्रा-पथ है, और अति, दुख की जननी है। अति, चिंता और तनाव पैदा करती है। अति स्वयं से बाहर जाना है, क्योंकि अति, साम्य को, समता को खोना है। स्वयं में ठहरने की भूमिका समता है। स्वयं में होना समता में हुए बिना संभव नहीं। समता अंतर्गमन का द्वार है। अति बहिर्गमन का। अति ही विषमता है। समता स्वास्थ्य है। विषमता अस्वास्थ्य। किंतु मनुष्य चित्त अस्वस्थ ही रहना चाहता है क्योंकि अस्वास्थ्य में ही उसका जीवन है, स्वास्थ्य की दिशा में गति तो उसकी मृत्यु को ही आमंत्रण है। इसलिए एक अति से ऊब जाता है, तो वह तत्क्षण दूसरी अति के प्रति आकर्षित हो जाता है। विराम का अवसर वह नहीं देता। अंतराल को क्षण भर भी रिक्त छोड़ने की भूल वह नहीं करता। रिक्तता उसके लिए संधातक है। तनाव की स्थिति सदा ही बनी रहे यही उसके लिए शुभ है। वह सदा दौड़ता रहे, दौड़ता ही रहे, यही उसके लिए प्राणदायी है। क्योंकि ठहरते ही, रुकते ही उसके दर्शन होते हैं जो कि आत्मा है। और आत्मा को पाने पर चित्त वैसे ही नहीं पाया जाता है, जैसे कि सूर्योदय होने पर रात्रि नहीं पाई जाती।
- रात्रि कुछ संन्यासियों के बीच था। उन्हें देखता था। उनके चित्त को देखता था। उनकी क्रियाओं को देखता था। वे सब कभी गृहस्थ थे। उस जीवन के विरोध और प्रतिक्रिया में अब वे संन्यासी हैं। उस जीवन को अब उन्होंने सब भांति उलटा कर लिया है। चित्त वही है, लेकिन दिशा विरोधी है। भोग छोड़ा तो त्याग को पकड़ लिया। धन छोड़ा तो दरिद्रता को पकड़ लिया। तब संसार की खोज में जाते थे, अब संसार से भागे जा रहे हैं। अति बदल गई है, किंतु अति फिर भी वहीं की वहीं है।
- एक मित्र हैं। वे कहते हैंः ‘स्त्री नरक का द्वार है।’ यह भी मैं जानता हूं कि कभी वे मानते थे कि स्त्री के अतिरिक्त और कोई स्वर्ग नहीं है। पहले वे स्त्री के लिए लड़ते थे, अब स्त्री से लड़ते हैं। किंतु उनके चित्त का केंद्र आज भी स्त्री बनी हुई है। काम (सेक्स)की ओर जावें या काम के विरोध में, दोनों ही स्थितियों में चित्त काम वासना पर ही घूमता रहता है। काम के विरोध में काम से मुक्ति नहीं है। जो स्त्री को स्वर्ग मानता है, वह तो कामुक है ही, जो उसे नरक मानता है वह भी कामुक ही है।
- शरीर के भोग में ही जाने वाले व्यक्ति हैं, और शरीर को पीड़ा देकर आनंद अनुभव करने वाले व्यक्ति भी हैं। किंतु स्मरण रहे कि दोनों ही देहवादी हैं। शरीर भोग ही उलटा होकर शरीर-योग बन जाता है। इंद्रिया-भोग ही इंद्रिय-दमन बन जाता है। चेतना दोनों ही अतियों में शरीर के तट से बंधी रहती है। इस भांति आत्मा की यात्रा न कभी हुई है, और न कभी हो ही सकती है।
- राग से विराग की अति पर चले जाना ज्ञान नहीं है।
- सुख से दुख की अति पर चले जाना संन्यास नहीं है।
- सत्य द्वंद्व में और अतियों के चुनाव में नहीं, वरन संयम में और समता में है।
- जीवन का रहस्य और उसे खोलने की कुंजी संयम है; संयम यानी चित्त की अतियों से मुक्ति। अतियों से मुक्त होना, चित्त से ही मुक्त हो जाना है।
- एक धनपति युवक थाः श्रोण। वह अपूर्व रूप, से सुंदर था। उसके वीरबहूटी से लाल तथा नवनीत से कोमल तलवे थे। उसके उन सुंदर तलवों पर मुलायम बाल भी उगे हुए थे। सम्राट बिंबिसार तक को उसे और उसके तलवों को देखने का कुतूहल हुआ था। श्रोण का जीवन वैभव-भोग में ही बीतता था। सुख ही सुख के सागर में वह तैरता था। किंतु फिर भी उसका चित्त शांत न था। आंनद के लिए वह भी लालायित था। जीवन अर्थ के ओर-छोर की खोज उसके मन को भी पीड़ित करती थी। धीरे-धीरे उसका चित्त सुखों से भी ऊब गया। सुख की संवेदनाएं भी बोथली हो गईं। धन, वैभव और भोग सब नीरस हो आया। ऊब की इसी चित्त-दशा में उसने बुद्ध के दर्शन किए और उनकी वाणी सुनी। उसके हृदय में नई अनुभूतियों की आशा जगी। वह विरक्त हो गया और उसने तप का मार्ग अपना लिया। चित्त ने भोग की प्रतिक्रिया में, विरोध में, दमन की दिशा सुझाई। वह भांति-भांति से शरीर को कष्ट देने लगा। मन बहुत अदभुत है। वही भोग की नई-नई विधियां
- खोजता है। वही शरीर-दमन और उत्पीड़न के नये-नये आविष्कार करता है। कामसूत्र भी वही रचता है, आत्म-हिंसक तपश्चर्या के मार्ग भी वही खोजता है। अतियों की खोज के लिए वह सदा ही अति-उत्सुक है। श्रोण भी आत्म-उत्पीड़न में लग गया। शरीर के घोर दमन में वह रस लेने लगा। भिक्षु साफ-सुथरे मार्गों पर चलते तो वह कुश-कंटकों से भरी भूमि पर ही चलता। शीत-ताप में शरीर को सताता। भूख-प्यास में शरीर को सताता। उसकी सुंदर देह सूख कर काली पड़ गई। उसके कोमल तलवों में घाव बन गए और रक्त बहने लगा। उसका शरीर अशक्त और रुग्ण हो गया। वह तपस्वी जो हो गया था!
- एक दिन बुद्ध तथाकथित तपस्वी श्रोण के पास गए। उसकी दशा देख उन्हें दया आनी स्वाभाविक ही थी। उन्होंने उससे बहुत प्रेम से पूछाः श्रोण! तूने कभी वीणा बजाई है? श्रोण को स्मरण आया। वह तो वीणा बजाने में बहुत कुशल था। उसने कहाः हां, भंते! तब बुद्ध ने पूछाः क्या तार बहुत ढीले हों तेा उनसे संगीत पैदा होता है? श्रोण बोलाः नहीं भंते! और यदि तार बहुत कसे हों तो? श्रोण ने कहाः तब भी नहीं, भंते! फिर संगीत कब पैदा होता है? यह सुन श्रोण जैसे निद्रा से जाग गया। उसकी आंखों से एक नशा विलीन हो गया। वह बोलाः भंते, वीणा के तारों से संगीत का जन्म तभी होता है, जब वे न तो अति ढीले हों और न अति कसे हों। उस सूक्ष्म संतुलन में ही संगीत पैदा होता है। बुद्ध ने कहाः फिर श्रोण, स्मरण रख कि जीवन के संगीत का भी नियम यही है।
- जीवन संगीत में हो, तो ही सत्य की अनुभूति होती है।
- समता, संतुलन, और संयम से संगीत पैदा होता है। चित्त अतियों में होता है तो विसंगति में होता है। वह जैसे ही अतियों के, द्वंद्वों के मध्य में ठहरता है, वैसे ही संगीत को पा लेता है। इस संगीत में आना ही स्वयं में आना है वही स्वास्थ्य है। वही सत्य है। वही धर्म है।
2 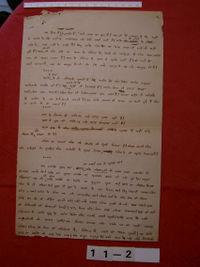
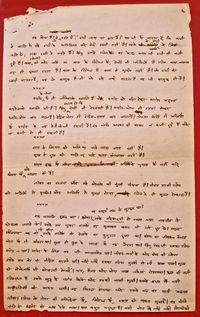
3 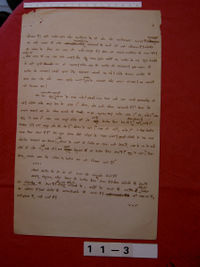
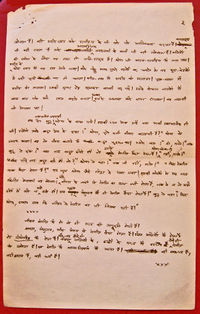
4 
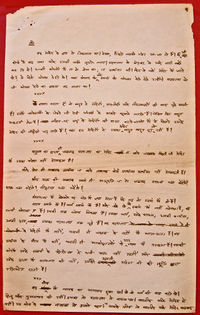
Prem Ke Swar (प्रेम के स्वर), chapter 29 - एक मंदिर के द्वार से निकल रहा था। देखा, सैकड़ों व्यक्ति भीतर आ-जा रहे हैं। मैं भी एक कोने में रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। परमात्मा को छोड़ कर वे और सारी बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में न तो प्रेम था, न प्रार्थना थी। फिर वे क्यों मंदिर में जा रहे थे? वे किसे धोखा दे रहे थे? क्या संसार को और स्वयं को धोखा देते देते उन्होंने परमात्मा को भी धोखा देने का साहस कर डाला था?
- स्मरण करता हूं तो बहुत-से मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों की याद मुझे आती है। उनमें जाने वालों के चेहरे भी मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। लेकिन फिर बहुत आश्चर्य होता है। जीवन भर प्रभु के मंदिरों की यात्रा करने वालों में से कितने उसके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ पाते हैं? क्या इन मंदिरों से उसका मंदिर बहुत बहुत दूर नहीं है?
- मनुष्य का हृदय ही जब तक परमात्मा का मंदिर न बने, तब तक किसी भी मंदिर में उसका प्रवेश नहीं हो सकता है।
- प्रेम ही जब तक प्रार्थना न बने तब तक कोई प्रार्थना प्रार्थना नहीं हो सकती है।
- सत्य की जब तक स्वयं ही अनुभूति न हो तब तक शास्त्र क्या करेंगे? शब्द क्या करेंगे? सिद्धांत क्या करेंगे?
- संसार भर में खोजने पर अंत में ज्ञात होता है कि वह तो स्वयं में ही है।
- सत्य स्वयं में है। धर्म स्वयं में है। जो उसे स्वयं में नही खोजता है, वह व्यर्थ खोजता है,
उसकी सब खोज मिथ्या है। उसका धर्म, उसके शास्त्र, उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा, उसका परमात्मा सब झूठे हैं।
- वह परमात्मा के मंदिरों में नहीं, अपनी ही वासना के घरों में आता-जाता है। वह प्रार्थना के मौन में नहीं, अपनी ही आकांक्षाओं के शब्द-जाल में भटकता है। उसकी आंखें उसके स्वार्थ के क्षितिज से कभी ऊपर नहीं उठतीं और उसके हृदय में परमात्मा की नहीं, उसकी अपनी अहंता की ही मूर्ति सदा प्रतिष्ठित रहती है।
- एक गांव में नानक का आगमन हुआ था। वे तो धर्म की बात करते थे, हिंदू और मुसलमान की नहीं। उनका तो परमात्मा से वास्ता था, मस्जिद और मंदिर से नहीं। उस गांव के नवाब ने उससे कहाः आपके लिए तो मस्जिद और मंदिर बराबर
- है, तो क्या आप आज मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को तैयार हैं? नानक ने बहुत आनंदित होकर कहाः जरूर, जरूर! परमात्मा की प्रार्थना में सम्मिलित होने से बड़ा आनंद और क्या है? फिर, नवाब, काजी और गांव के बहुत-से लोग मस्जिद गए। सभी नानक की नमाज देखना चाहते थे। मस्जिद में पहुंच कर काजी और नवाब और उनके साथी नमाज अदा करने लगे किंतु नानक एक कोने में खड़े ही गए और चुपचाप उनकी ओर देखने लगे। उनको इस भांति खड़ा देख कर नवाब और काजी को बहुत क्रोध आने लगा। वे बीच बीच में नानक की ओर क्रोध से देख भी लेते थे। फिर किसी भांति जल्दी-जल्दी उन्होंने नमाज पूरी की और सब नानक पर टूट पड़े। वे नानक को धोखेबाज और वचन तोड़ने वाला कहने लगे। नवाब ने क्रोध से आंखें लाल करके नानक को डांटा और कहाः आपने नमाज क्यों नहीं की? आप नमाज में सम्मिलित क्यों नहीं हुए? नानक यह सब देख खूब हंसने लगे और बोलेः मैं तो नमाज में सम्मिलित होने आया था, लेकिन जब आपने ही नमाज नहीं पढ़ी तो मैं चुपचाप दूर खड़ा आपके खेल को देखता रहा। और करता भी क्या? आप सबका ध्यान तो मेरी ओर था। परमात्मा की ओर तो किसी का भी ध्यान नहीं था। यह कैसी इबादत? यह कैसी प्रार्थना? परमात्मा के निकट इस भांति कैसे हुआ जा सकता है?
- मैं भी मंदिरों के, मस्जिदों के, गिरजों के कोनों में खड़े होकर देखता रहा हूं। और जो देखा, उससे ज्यादा असत्य मनुष्य के जीवन में और कुछ भी नहीं पाया। जब धर्म ही असत्य हो तो शेष सब अपने-आप ही असत्य हो जाता है। मनुष्य का सब कुछ असत्य हो गया है क्योंकि उसका परमात्मा असत्य है, उसकी प्रार्थना असत्य है। परमात्मा जीवन का आधार है और केंद्र है, और यदि वही असत्य है तो फिर और क्या सत्य हो सकता है?
5 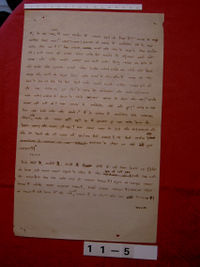
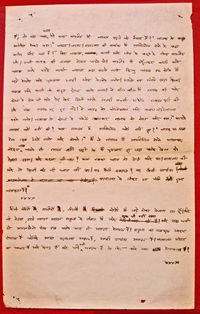
6 
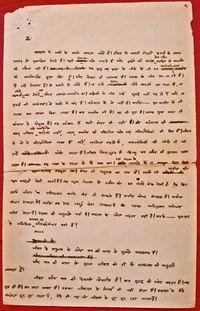
Prem Ke Swar (प्रेम के स्वर), chapter 31 - आकाश में वर्षा के पहले बादल घिरे हैं। ग्रीष्म में प्यासी हो उठी पृथ्वी के प्राण आनंद से पुलकित हो रहे हैं। पक्षी मंगल-गीत गा रहे हैं और वृक्षों की आंखें प्रेम और प्रतीक्षा से बादलों को निहार रही हैं। एक पुराने बड़-वृक्ष के नीचे मैं भी इस आनंदोत्सव में सम्मिलित हुआ बैठा हूं। निकट ही जनपथ है। उसपर से लोग आ-जा रहे हैं। मैं उन्हे देखता हूं। वे अपने में घिरे हैं। न उन्हें ऊपर घिरे बादलों का पता है, न नीचे हो रहे इस विराट स्वागत-समारोह का। पक्षियों के गीत उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहे और न पृथ्वी की प्रार्थनाएं। वे अपने में बंद हैं। वर्तमान में वे नहीं हैं। अतीत, मृत अतीत में ही उनका मन यात्रा किए जाता है। मन अतीत ही है। वह भी मृत है उसका मुख सदा ही वर्तमान से विमुख है। वह वर्तमान में कभी होता ही नहीं। उसे वर्तमान की सतत जीवंत और अपरिचित घड़ियां नहीं, वरन अतीत की परिचित और जड़ परिस्थितियां ही प्रिय हैं। जीवन में तो वे परिस्थितियां अब नहीं, इसलिए स्मृति में, मन-स्थितियों की भांति ही वह उन्हें जिये जाता है। जीवन नित-नूतन है, किंतु मन सदैव ही पुरातन बना रहता है।
- एक राजा के महल में मैं गया था। उस महल के तलघरे में न मालूम किस किस सदी का कूड़ा-कबाड़ इकट्ठा था। ऐसा ही मनुष्य का मन है। उसमें भी अतीत की धूल इकट्ठी होती रहती है। यह धूल चेतना के दर्पण को इस भांति ढंक लेती है कि फिर उसमें जीवन के प्रतिफलन बनने बंद ही हो जाते हैं। अतीत बोझ हो जाता है। अतीत बंधन हो जाता है। अतीत एक ऐसा जादुई घेरा हो जाता है कि उसका अतिक्रमण असंभव प्रतीत होता है। चेतना की अमुक्ति यही है। आत्मा के लिए जड़ता यही है। मन के, मृत मन के अतिरिक्त आत्मा पर और कोई बंधन कहां हैं?
- जीवन के अनुभव के लिए मन की कारा से मुक्ति आवश्यक है।
- मन की कारा से मुक्त जीवन को ही मैं परमात्मा की अनुभूति जानता हूं।
- जीवन और मन की दिशाएं विपरीत हैं। मन मृत्यु की ओर बहता है। वह मृत ही है। मन सदा बासा है। उसका जीवंत से संपर्क ही नहीं होता है। प्रकाश से जैसे अंधेरा दूर-दूर रहता है, ऐसे ही वह भी जीवन से दूर-दूर रहा आता है।
- श्रावस्ती का मृगार श्रेष्ठ करोड़ों मुद्राओं का स्वामी था। वह मन में अपनी मुद्राएं ही गिनता रहता। उनकी गणना में ही वह जीता था। वही उसका जीवन था। उनमें ही उसके प्राण थे। उस घेरे के बाहर न उसकी दृष्टि थी, न अनुभूति थी। सोते और जागते मुद्राओं का स्वप्न ही उसे सुलाए रखता था। वह जैसे होश में ही नहीं था। मुद्राओं के सम्मोहन में मूर्च्छित वह होश में होने के भ्रम में ही होता था। एक दिन वह भोजन करने बैठा तो उसकी पुत्रवधु ने पूछाः भोजन कैसा है, तात? कोई त्रुटि तो नहीं? त्रुटि और विशाखा सी चतुर बहू से? मृगार कौर चबाता हंस पड़ाः किंतु तुम ऐसा क्यों पूछती हो, आयुष्मती? तुमने तो सदा ही ताजे भोजन से मुझे तृप्त किया है? यह सुन उसकी पुत्रवधु ने दृष्टि नीची कर बहुत दुख से कहाः यही तो आपका भ्रम है। मैं आज तक आपको बासा भोजन ही खिलाती रही हूं। मेरी प्रबल इच्छा है कि आपको ताजे व्यंजन खिलाऊं, किंतु विवश हूं, क्योंकि ताजे भोजन करने को आप तैयार ही नहीं हैं! मृगार के हाथ का कौर हाथ में ही रह गया और उसने कहाः यह क्या कह रही हो शुभे। विशाखा ने कहाः ठीक ही कहती हूं। मन जिसका बासा है, उसका सब-कुछ, सारा जीवन ही बासा हो जाता है। मन जिसका मृत है, वह जीवित होते हुए भी जीवित नहीं रह जाता है।
- वर्तमान में, सदा वर्तमान में जो सजग है, सचेत है, सावधान है, वही जाग्रत है, वही जीवित है। वही सत्ता से संबंधित है। न तो अतीत है, न भविष्य है। जो है, वह अभी है और यहीं है। अस्तित्व सदा वर्तमान में है। मन कभी भी वर्तमान में नहीं है। इसीलिए मन सत्ता को जानने में असमर्थ हो जाता है। सत्य की राह पर वह इसीलिए बाधा बन जाता है। सत्य को पाना है तो मन को छोड़ना होता है। मन को छोड़ने की विधि क्या है? वह विधि हैः अतीत और भविष्य के सम्मोहन को तोड़ कर वर्तमान के सत्य के प्रति जागना जो है, जो चारों ओर है, जो भीतर-बाहर है, उसके प्रति सहज और सतत जागरूकता से मन क्रमशः विसर्जित हो जाता है, और तब मन की मृत्यु पर उस मौन का जन्म होता है जो कि सत्य के अज्ञात सागर में यात्रा के लिए नौका बन जाता है।
7