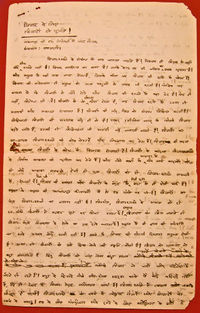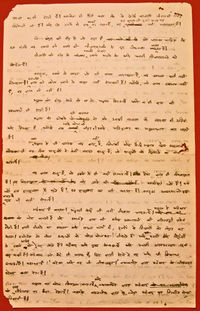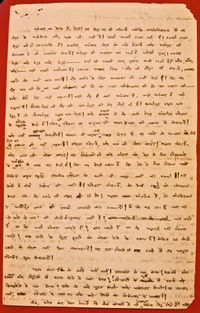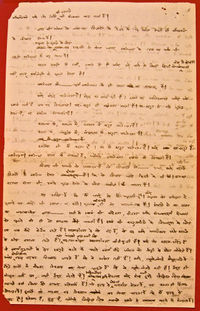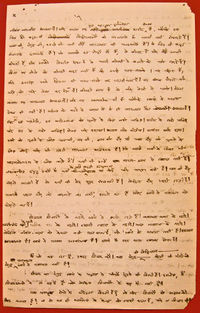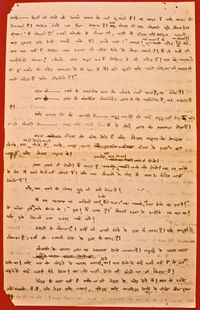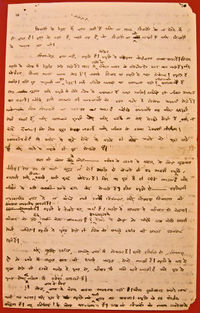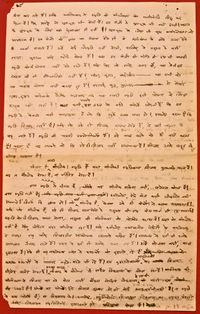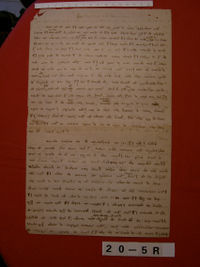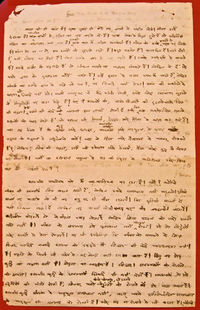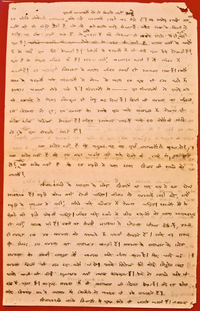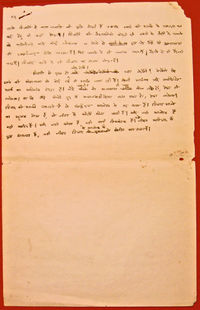| sheet no |
original photo |
enhanced photo |
Hindi
|
| 1R |
 |
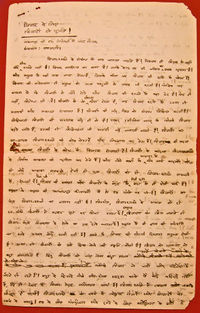 |
विचार के लिए
विचारों से मुक्ति !
जबलपुर की एक संगोष्ठी में प्रगट विचार
संकलन : रमाअरविंद
- विचार-शक्ति के संबंध में आप जानना चाहते हैं? निश्चय ही विचार से बड़ी और कोई शक्ति नहीं। विचार व्यक्तित्व का प्राण है। उसके केंद्र पर ही जीवन का प्रवाह घूमता है। मनुष्य में वही सब प्रकट होता है, जिसके बीज वह विचार की भूमि में बोता है। विचार की सचेतना ही मनुष्य को अन्य पशुओं से पृथक भी करती है। लेकिन यह स्मरण रहे कि विचारों से घिरे होने और विचार की शक्ति में बड़ा भेद है। भेद ही नहीं, विरोध भी है। विचारों से जो जितना घिरा होता है, वह विचार करने से उतना ही असमर्थ और अशक्त हो जाता है। विचारों की भीड़ चित्त को अंततः विक्षिप्त करती है। विक्षिप्तता विचारों की अराजक भीड़ ही तो है! शायद इसीलिए जगत में जितने विचार बढ़ते जाते हैं, उतनी ही विक्षिप्तता भी अपनी जड़ें जमाती जाती है। विचारों का आच्छादन विचार-शक्ति को ढांक लेता है और निष्प्राण कर देता है। विचार का सहज स्फुरण विचारों के बोझ से निःसत्व हो जाता है। विचारों के बादल विचार-शक्ति के निर्मल आकाश को धूमिल कर देते हैं। जैसे वर्षा में आकाश में घिर आए बादलों को ही कोई आकाश समझ ले, ऐसी ही भूल विचारों को ही विचार-शक्ति समझने में हो जाती है। फिर भी विचार की क्षमता और विचारों के संग्रह में ऐसी भूल सदा ही होती आई है। मनुष्य के अज्ञान की आधारभूत शिलाओं में से एक भ्रांति यह भी है। विचारों का संग्रह विचार-शक्ति का प्रमाण नहीं है। विपरीत विचार-शक्ति के अभाव को ही इस भांति विचारों से भर कर पूरा कर लिया जाता है। प्रसुप्त विचारणा को बिना जगाए ही विचार-संग्रह विचारणा के होने का भ्रम देने लगता है। अज्ञान में ही ज्ञान की अहं-पूर्ति का इससे आसान कोई मार्ग नहीं है। स्वयं में विचार की जितनी रिक्तता अनुभव होती है, उतनी ही विचारों से उसे छिपा लेने की प्रवृत्ति होती है। विचार को जगाना तो बहुत श्रमसाध्य है; किंतु विचारों को जोड़ लेना बहुत सरल है, क्योंकि विचार तो चारों ओर परिवेश में तैरते ही रहते हैं। समुद्र के किनारे जैसे सीप-शंख इकट्ठा करने में कोई कठिनाई नहीं है, ऐसे ही संसार में विचार-संग्रह अति सरल कार्य है। विचार-शक्ति है स्वरूप, जब कि विचार हैं पराए। विचार-शक्ति को स्वयं में खोजना होता है और विचारों को स्वयं के बाहर। एक के लिए अंतर्मुखता और दूसरे के लिए बहिर्मुखता के द्वारों से
|
| 1V |
 |
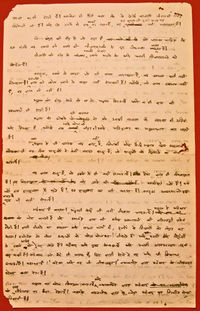 |
- यात्रा करनी होती है। इसलिए ही मैंने कहा कि दोनों यात्राएं भिन्न ही नहीं, विरोधी भी हैं। और जो उनमें से एक यात्रा पर जाता है, वह इस कारण ही दूसरी यात्रा पर नहीं जा सकता है।
- विचार-संग्रह की दौड़ों में जो पड़ा है उसे जानना चाहिए कि इस भांति वह स्वयं ही स्वयं की विचार-शक्ति से दूर निकलता जाता है।
- विचारों की भीड़ में व्यक्ति अंततः स्वयं अपने को और अपनी विचार-शक्ति को खो देता है।
- वस्तुतः स्वयं से बाहर जो भी पाया जा सकता है, वह स्वरूप कभी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान की खोज स्वयं से बाहर नहीं हो सकती है; क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप नहीं है, वह ज्ञान ही नहीं है।
- अज्ञान को ढांक लेने से न तो अज्ञान मिटता है और न ही ज्ञान की उपलब्धि ही होती है।
- अज्ञान को ढांकने की बजाय तो उसे उसकी नग्नता में जानना ही उचित और हितकर है, क्योंकि तब उसकी बोध की पीड़ा ही उसके अतिक्रमण का अनुसंधान बन जाती है।
- क्या अज्ञान से भी घातक वह ज्ञान नहीं है जिसकी ओट में अज्ञान छिप सकता है? निश्चय ही वह मित्र शत्रुओं से कहीं ज्यादा शत्रु है जो शत्रुओं को छिपाने का कार्य करता है।
- वह ज्ञान शत्रु है जो स्वयं से ही नहीं जन्मता है। ऐसा ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान को पाने की आकांक्षा क्यों है? हम क्यों इस मृगतृष्णा में पड़ते हैं? इस मृगतृष्णा का भी कारण है। वस्तुतः अकारण तो इस जगत में कुछ भी नहीं होता है।
- अहंकार है कारण। अज्ञानी कोई भी नहीं दिखना चाहता है। अज्ञान से अहंकार को चोट लगती है और इसलिए ज्ञान की शीघ्र उपलब्धि की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। ज्ञानी दिखने का सस्ता और सरल मार्ग है दूसरे के विचारों का संग्रह कर लेना। इसलिए तो लोग शास्त्रों को घोल-घोल कर पी जाते हैं और शब्दों और सिद्धांतों से स्वयं को आकंठ भर लेते हैं। तब अहंकार और पुष्ट हो जाता है और उसकी साज-सज्जा खूब बढ़ जाती है। अहंकार तो वैसे ही घातक है, फिर ज्ञानी होने से वह और भी विषाक्त हो जाता है। कहावत है, करेला और वह भी नीम चढ़ा! तथाकथित ज्ञान अहंकार को नीम चढ़ा करेला बना देता है।
- अज्ञान का बोध विनम्रता लाता है और तथाकथित ज्ञान अहंकार को राज-सिंहासन पर बैठा देता है, जब कि वास्तविक ज्ञान के लिए अहंकार का विलीन होना अनिवार्य है।
|
| 2R |
 |
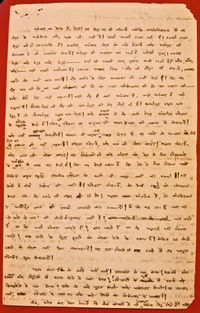 |
- अहंकार का केंद्र है संग्रह। वह संग्रह पर ही जीता है, क्योंकि आत्यंतिक रूप में वह संग्रह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसकी अपनी सत्ता नहीं है। उसकी सत्ता संग्रह की ही उप-उत्पत्ति है। इसलिए अहंकार संग्रह को गति देता है और असंग्रह की संभावना से ही भयभीत होता है। असंग्रह की अवस्था का अर्थ है उसकी मृत्यु। इसलिए संग्रह होता है। और संग्रह, और संग्रह..ऐसी ही उसकी सतत पुकार बनी रहती है। और, और, और..यही उसकी अभीप्सा है। इसलिए जब तक चित्त और की दौड़ में होता है तब तक स्वयं को नहीं जाना पाता। दौड़ जानने के लिए अवकाश ही नहीं देती। फिर यह दौड़ धन की हो या धर्म की, पद की हो या यश की, ज्ञान की हो या त्याग की, इससे कोई भेद नहीं पड़ता है। जहां दौड़ है वहां अहंकार है, जहां अहंकार है वहां अज्ञान है। विचार-संग्रह की दौड़ भी धन-संग्रह की दौड़ जैसी ही है। धन-संग्रह स्थूल धन-संग्रह है, तो विचार-संग्रह सूक्ष्म धन-संग्रह। और ध्यान रहे कि सभी संग्रह आंतरिक दरिद्रता के द्योतक होते हैं। भीतर की दरिद्रता का अनुभव ही बाहर के धन की तलाश में ले जाता है। और यहीं मूल भूल शुरू हो जाती है। पहला ही चरण गलत दिशा में पड़ जाए तो गंतव्य के ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। दरिद्रता भीतर है और धन की खोज बाहर! यह विसंगति ही सारे जीवन को रेत से तेल निकालने के अर्थहीन श्रम में नष्ट कर देती है। फिर यह हो भी सकता है कि रेत से तेल निकल आवे, लेकिन बाह्य समृद्धि आंतरिक दरिद्रता को कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। उन दोनों में कोई संबंध ही नहीं। दरिद्रता भीतर है, तो ऐसी समृद्धि को खोजना होगा जो स्वयं भी भीतर की ही हो। अज्ञान आंतरिक है, तो आंतरिक रूप से आविर्भूत ज्ञान ही उसकी समाप्ति बन सकता है। मैं जो कह रहा हूं, क्या वह दो और दो चार की भांति ही सुस्पष्ट नहीं है? धन चाहते हैं या कि धनी दिखना चाहते हैं? ज्ञान चाहते हैं या कि अज्ञानी नहीं दिखना चाहते? सब भांति के संग्रह दूसरों को धोखा देने के उपाय हैं। लेकिन इस भांति स्वयं को धोखा नहीं दिया जा सकता है। यह सत्य दिखते ही दृष्टि में एक आमूल परिवर्तन शुरू हो जाता है।
- अज्ञान सत्य है तो उससे भागें नहीं। पलायन से क्या होगा? शास्त्रों, शब्दों और सिद्धांतों में शरण लेने से क्या होगा? विचारों के धुएं में स्वयं को छिपा लेने से क्या होगा? उससे तो और घुटन होगी, और घबराहट होगी। वह उपचार नहीं, उपचार के नाम पर और बड़े रोगों को निमंत्रण दे आना है।
- अनेक बार ऐसा होता है कि वैद्य बीमारी से भी ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं और
|
| 2V |
 |
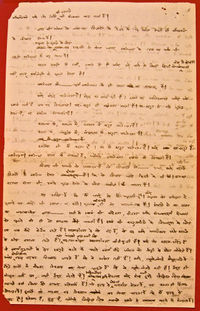 |
- औषधियां नये रोगों की उत्पत्ति कीशृंखला बन जाती हैं।
- ज्ञान की खोज के नाम पर विचारों के संग्रह में पड़ जाना ऐसी ही औषधि के शिकार होना है।
- अज्ञान से मुक्ति के लिए शास्त्रों से बंध जाना, स्वतंत्रता के नाम पर और भी गहरी परतंत्रता में पड़ जाना है।
- सत्य शब्दों में नहीं, स्वयं में है। और उसे पाने के लिए किसी तंत्र से बंधना नहीं, वरन सर्व तंत्रों से मुक्त होना है।
- स्वतंत्रता में..पूर्ण स्वतंत्रता में ही..सत्य का साक्षात है।
- संग्रह परतंत्रता है। संग्रह का अर्थ ही है स्वयं पर अविश्वास और जो स्वयं नहीं है उस पर विश्वास! पर-श्रद्धा ही परतंत्रता लाती है। पर-श्रद्धा से जो मुक्त होता है, वह स्वतंत्र हो जाता है।
- शास्त्र में, शास्ता में, शासन में श्रद्धा परतंत्रता है।
- शब्द में, सिद्धांत में, संप्रदाय में श्रद्धा परतंत्रता है।
- इसलिए ही मैं कहता हूं: पर में श्रद्धा करना परतंत्रता है; और स्व-श्रद्धा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सत्य में ले जाती है।
- विचार की शक्ति को जगाना हो तो विचारों से..उधार और पराए विचारों से..स्वतंत्र होना होगा, फिर वे विचार चाहे किसी के भी हों। उनका पराया होना ही उनसे मुक्त होने के लिए पर्याप्त कारण है।
- यह उचित है कि मैं जानूं कि मैं अज्ञानी हूं और अज्ञान को शीघ्रता से भूलने का कोई भी उपाय न करूं। भूलने की दृष्टि ही तो आत्मवंचक है। संपत्ति हो या सत्ता या तथाकथित ज्ञान, सभी में स्वयं की दरिद्रता, दीनता और अंधकारपूर्ण रिक्तता को भूलने की ही तो साधना चलती है। स्वयं की वस्तुस्थिति के विस्मरण के लिए हम सब कैसे बेचैन रहते हैं! आत्महीनता से जो भरे हैं, वे पद, अधिकार और शक्ति के लिए पागल रहते हैं। क्या आपको ज्ञात नहीं कि महत्वाकांक्षा आत्महीनता की ही पुत्री है? आत्मदरिद्र हैं वे जो स्वर्ण-मुद्राओं के ढेर इकट्ठे करने में अपने स्वर्ण जैसे जीवन को मिट्टी के मोल खो देते हैं। अपंग डोलियों पर पहाड़ चढ़ कर दिखाना चाहते हैं कि वे अपंग नहीं हैं! और लूले-लंगड़े विद्युत गति से दौड़ते यानों में बैठ कर विश्वास कर लेना चाहते हैं कि वे लूले-लंगड़े नहीं हैं! तैमूर ही लंगड़ा नहीं था, सभी तैमूर लंगड़े हैं! एलेक्जेंडर, हिटलर और शेष सभी विक्षिप्त चित्त व्यक्ति इसी नियम की साकार प्रतिमाएं हैं। जो मृत्यु से जितना भयभीत होता है, वह उतना ही हिंसक हो जाता है। दूसरों को मार कर वह विश्वास कर लेना चाहता है कि मैं मृत्यु के ऊपर हूं। शोषण है, युद्ध है, क्योंकि विक्षिप्त चित्त व्यक्ति स्वयं से पलायन करने में संलग्न हैं।
|
| 3R |
 |
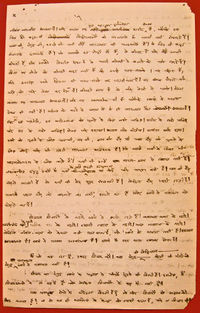 |
- जीवन नारकीय हो गया है, और समाज मृत, सड़ा हुआ, दुर्गंध देता शरीर हो गया है, क्योंकि हम चित्त की बहुत सी विक्षिप्तताओं को पहचानने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। सत्ता की, संग्रह की, शक्ति की सभी दौड़ें पागलपन की अवस्थाएं हैं। ये चित्त की बहुत संघातक रुग्णताएं हैं। जो व्यक्ति इन दौड़ों में हैं, वे बीमार हैं। और जहां उनकी बीमारी है, ठीक उसकी विपरीत दिशा में वे अपनी बीमारी से बचने को भागे जा रहे हैं, बिना सोचे कि बीमारी बाहर नहीं है कि उससे भागा जा सके! वह भीतर है। इसलिए उससे कितना ही भागा जाए वह सदा ही साथ है। यह बोध दौड़ने की गति को तेज कर देता है। बीमारी साथ है तो और तेजी से भागो। अंततः भागना एक पागलपन हो जाता है। और स्वाभाविक ही है, क्योंकि स्वयं से भागना संभव ही नहीं। असंभव को करने के प्रयास से ही पागलपन पैदा हो जाता है। फिर इस अशांति और अति तनाव को भूलने के लिए नशे चाहिए। शरीर के नशे चाहिए और मन के नशे चाहिए..सेक्स और शराब; भजन और कीर्तन; प्रार्थना और पूजा! स्वयं को भूलने के लिए धन की, पद की, ज्ञान की दौड़ है। अब दौड़ को भूलने के लिए कोई भी गहरी मादकता आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति धर्म के निकट भी आत्म-विस्मरण के लिए आते हैं। धर्म भी उन्हें एक मादक द्रव्य से ज्यादा नहीं है। तथाकथित समृद्ध देशों में धर्म के प्रति बढ़ती उत्सुकता का कोई और कारण नहीं है। धन की दौड़ तोड़ने लगती है तो धर्म की दौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन दौड़ जारी रहती है। जब कि प्रश्न दौड़ को बदलने का नहीं, ठहरने का है और स्वयं से पलायन को छोड़ने का है।
- विचारक विचारों के सहारे स्वयं से भागे रहते हैं; कलाकार कला के सहारे; राजनैतिक सत्ता के सहारे; धनिक धन के सहारे; त्यागी त्याग के सहारे; भक्त भगवान के सहारे। लेकिन जीवन-सत्य को केवल वही जान पाता है जो स्वयं से भागता नहीं है। पलायन अस्वास्थ्य है। स्वयं से भागना अस्वास्थ्य है। स्वयं में ठहर जाना स्वस्थ होना है।
- मैं जो कह रहा हूं, उस पर विचार करें। क्या संग्रह की विक्षिप्तता..किसी भी भांति के संग्रह की विक्षिप्तता..स्वयं से पलायन नहीं है?
- विचार का संग्रह स्वयं के अज्ञान से आंखें मूंदने की विधि है। इसलिए मैं विचार-शक्ति के तो पक्ष में हूं, लेकिन विचारों के पक्ष में नहीं हूं।
- क्या धनाढ्य होने से दरिद्रता मिटती है? तो फिर विचारों से अज्ञान कैसे मिट सकता है? न तो धन व्यक्तित्व के केंद्र को स्पर्श करता है और न विचार ही।
|
| 3V |
 |
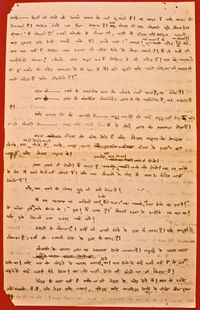 |
- संपत्ति..किसी भी भांति की संपत्ति..आत्मा को नहीं छू पाती है। वह बाहर और बाहर ही हो सकती है। लेकिन उससे भ्रम पैदा हो जाता है। कल संध्या ही एक भिखारी मुझे मिला। वह बोला, मैं भिखारी हूं। उसकी आंखों में दीनता थी, वाणी में दीनता थी। लेकिन उसकी बात सुन कर मुझे हंसी आ गई और मैंने उससे कहा, पागल! क्या कहता है कि तू दरिद्र है, भिखारी है? तेरे पास धन नहीं है, क्या इतना ही दरिद्र होने के लिए काफी है? मैं तो उन्हें भी भलीभांति जानता हूं जिनके पास बहुत धन है, लेकिन वे भी दरिद्र हैं! धन से ही तू स्वयं को दरिद्र समझता हो तो भूल है। रही दूसरी और गहरी दरिद्रता की बात, सो सभी दरिद्र हैं और भिखमंगे हैं।
- सत्य को, स्वयं के आत्यंतिक सत्य को जिसने नहीं जाना है, वह दरिद्र है।
- ज्ञान से, स्वयं में अंतर्निहित ज्ञान से जो अपरिचित है, वह अज्ञान में है।
- और स्मरण रहे कि वस्त्रों से, समृद्ध वस्त्रों से कोई समृद्ध नहीं होता; और न ही विचारों से, उधार और पराए विचारों से कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है।
- वस्त्र दीनता को ढांक लेते हैं और विचार अज्ञान को। लेकिन जिनके पास गहरी देखने वाली आंखें हैं, उनके समक्ष वस्त्र दीनता के प्रदर्शन बन जाते हैं और विचार अज्ञान के।
- आप स्वयं ही देखिए। मैं कहता हूं, इसलिए मत मान लेना। स्वयं ही सोचो, जागो और देखो। क्या हम वस्त्रों के मोह में स्वयं को ही नहीं खो रहे हैं? और क्या विचारों के मोह में सत्य से वंचित नहीं हो गए हैं?
- और क्या स्वयं को खोकर कुछ भी पाने योग्य है?
- मैं एक महाराजा का अतिथि था। उनसे मैंने कहा, क्या आपको भी राजा होने का भ्रम है? वे चकित हुए और बोले, भ्रम? मैं राजा हूं! कितनी दृढ़ता से उन्होंने यह कहा था और मुझे कितनी दया उन पर आई थी!
- पंडितों से मिलता हूं, उन्हें भी ज्ञानी होने के भ्रम में पाता हूं। साधुओं से मिलता हूं, उन्हें भी त्यागी होने के भ्रम में पाता हूं।
- विचारों के कारण ज्ञान का आभास होने लगता है, समृद्धि के कारण सम्राट होने का, धन को छोड़ने के कारण त्यागी होने का। धन से कोई धनी नहीं है तो धन छोड़ने से कोई त्यागी कैसे होगा? वह तो धनी होने की भ्रांति का ही विस्तार है।
- संग्रह में सत्य नहीं है और न ही संग्रह के छोड़ देने में। सत्य तो उसके प्रति जागने में है, जो संग्रह और त्याग, परिग्रह और अपरिग्रह, दोनों के पीछे बैठा हुआ है।
|
| 4R |
 |
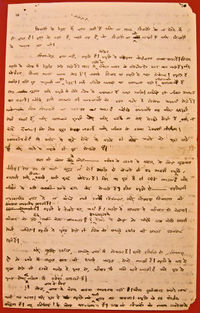 |
- विचारों के संग्रह में ज्ञान नहीं है और न मात्र विचारों के न होने में ही ज्ञान है। ज्ञान तो वहां है, जहां वह है, जो विचारों का भी साक्षी है और विचारों के अभाव का भी।
- विचार-संग्रह ज्ञान नहीं, स्मृति है। लेकिन स्मृति के प्रशिक्षण को ही ज्ञान समझा जाता है। विचार स्मृति के कोष में संगृहीत होते जाते हैं। बाहर से प्रश्नों का संवेदन पाकर वे उत्तेजित हो उत्तर बन जाते हैं, और इसे ही हम विचार करना समझ लेते हैं। जब कि विचार का स्मृति से क्या संबंध? स्मृति है अतीत, बीते हुए अनुभवों का मृत संग्रह। उसमें जीवित समस्या का समाधान कहां? जीवन की समस्याएं हैं नित नूतन, और स्मृति से घिरे चित्त के समाधान हैं सदा अतीत। इसलिए ही जीवन उलझन बन जाता है, क्योंकि पुराने समाधान नयी समस्याओं को हल करने में नितांत असमर्थ होते हैं। चित्त चिंताओं का आवास बन जाता है, क्योंकि समस्याएं एक ओर इकट्ठी होती जाती हैं और समाधान दूसरी ओर। और उनमें न कोई संगति होती है और न कोई संबंध। ऐसा चित्त बूढ़ा हो जाता है और जीवन से उसका संस्पर्श शिथिल। स्वाभाविक ही है कि शरीर के बूढ़े होने के पहले ही लोग अपने को बूढ़ा पाते हैं और मरने के पहले ही मृत हो जाते हैं।
- सत्य की खोज के लिए, जीवन के रहस्य के साक्षात के लिए युवा मन चाहिए, ऐसा मन जो कभी बूढ़ा न हो। अतीत से बंधते ही मन अपनी स्फूर्ति, ताजगी और विचार-शक्ति, सभी कुछ खो देता है। फिर वह मृत में ही जीने लगता है और जीवन के प्रति उसके द्वार बंद हो जाते हैं। चित्त स्मृति से, स्मृति रूपी तथाकथित ज्ञान से न बंधे, तभी उसमें निर्मलता और निष्पक्ष विचारणा की संभावना वास्तविक बनती है। स्मृति से देखने का अर्थ है, अतीत के माध्यम से वर्तमान को देखना। वर्तमान को ऐसे कैसे देखा जा सकता है? सम्यक रूप से देखने के लिए तो आंखें सब भांति खाली होनी चाहिए। स्मृति से मुक्त होते ही चित्त को सम्यक दर्शन की क्षमता उपलब्ध होती है।
- और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में ले जाता है। दृष्टि निर्मल हो, निष्पक्ष हो, तो स्वयं में प्रसुप्त ज्ञान की शक्ति जाग्रत होने लगती है। स्मृति के भार से मुक्त होते ही दृष्टि अतीत से मुक्त हो वर्तमान में गति करने लगती है, और मृत से मुक्त होकर वह जीवन में प्रवेश पा जाती है।
- ज्ञान के लिए ज्ञान का भंडार बनाना आवश्यक नहीं। वैसा दुव्र्यवहार अपने साथ कभी मत करना। भूल से स्मृति को कभी ज्ञान मत मानना। स्मृति तो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। वह विचार के लिए आच्छादन है। अब तो विचारों को स्मरण रखने वाले
|
| 4V |
 |
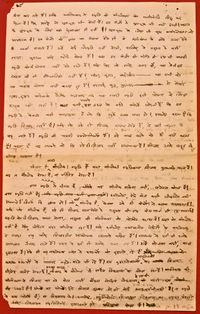 |
- यंत्र बन गए हैं। उनके आविष्कार ने स्मृति की यांत्रिकता को भलीभांति सिद्ध कर दिया है। फिर आप से तो भूल-चूक भी होती है, इन यंत्रों से भूल-चूक भी नहीं होती। असल में भूल-चूक के लिए वहां गुंजाइश ही नहीं। भूल-चूक के लिए भी कुछ अयांत्रिकता आवश्यक है। ज्ञान का भोजन देते ही वे यंत्र तत्संबंध में सारे उत्तर देने में ज्यादा कुशल और भरोसे के योग्य हो जाते हैं। क्या उन यंत्रों की भांति ही हम भी अपनी स्मृति को भोजन नहीं देते रहते हैं? और फिर जो हमारे उत्तर हैं, क्या वे भी इस भोजन की ही प्रतिध्वनियां नहीं हैं? गीता, कुरान, बाइबिल, क्या सभी को हम अपना भोजन नहीं बनाए हुए हैं? महावीर, बुद्ध, मोहम्मद से लेकर सुबह-सुबह आने वाले दैनिक अखबार तक क्या हमारी स्मृति इसी भोजन के लिए उत्सुक नहीं रहती है? क्या कभी आपने इस तथ्य के प्रति आंखें खोली हैं कि इस स्मृति से केवल वही आ सकता है जो उसमें डाला गया हो? इसलिए कहता हूं कि स्मृति विचार नहीं है। और जो उसे ही विचार समझ लेते हैं वे बड़ी जड़ता में पड़ जाते हैं। स्मृति की अपनी उपयोगिताएं हैं। उसे नष्ट करने को मैं नहीं कहता हूं। कहता हूं, यह समझने को कि उसे ही विचार नहीं समझना है। विचार उससे बहुत ही भिन्न आयाम है।
- विचार है सदा मौलिक। स्मृति है सदा यांत्रिक। स्मृतिजन्य विचार पुनरुक्ति मात्र है। वह न मौलिक होता है, न जीवंत होता है।
- ज्ञान स्मृति से भिन्न है, क्योंकि वह यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, सचेतन बोध है। ज्ञान स्मृति नहीं है। इसलिए ऐसे यंत्र कभी विकसित नहीं हो सकते हैं, जिनमें ज्ञान हो। जो कार्य यांत्रिक है, केवल उसे ही यंत्रों से कराया जा सकता है, और जो यांत्रिक है, उसे ही विचार मान लेने से मनुष्य एक यंत्र मात्र ही रह जाता है। स्मृति को ही विचार मान लेना मनुष्य की यांत्रिकता को घोषित करना है। प्रज्ञा तो यांत्रिक नहीं है, किंतु पांडित्य सदा यांत्रिक रहा है। इसलिए तथाकथित पंडितों के मस्तिष्क से ज्यादा जड़ और विचारहीन मस्तिष्क खोजना कठिन है। समस्या के पूर्व ही उनके समाधान तैयार रहते हैं। प्रश्न के पूर्व ही उनके उत्तर तय हैं। उन्हें सोचना नहीं, मात्र दोहराना है। ऐसे ही जड़ मस्तिष्क सदा से शास्त्रों को दोहराते रहे हैं और शास्त्रों के नाम पर लड़ते-मरते भी रहे हैं। इन दोहराने वाले मस्तिष्क को विचार विद्रोह प्रतीत होता है। उनका आग्रह विचार के विरोध में सदैव विश्वास के लिए रहा है। मस्तिष्क की यांत्रिकता से विचार का तो मेल नहीं बैठता, लेकिन विश्वास से उसकी पटरी खूब बैठ जाती है। अंधे का अंधे से मिलन सुखद हो तो कोई आश्चर्य नहीं। न स्मृति के पास आंखें हैं, न विश्वास के पास। इसलिए स्मृति-निर्भर विचारणा विश्वास का सहारा मांगती है, और विश्वास स्मृति-निर्भर पुनरुक्ति से परिपुष्ट होता है।
|
| 5R |
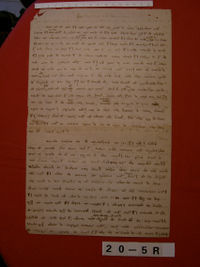 |
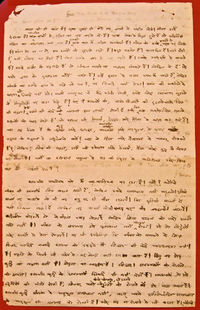 |
- आज की ही बात है, सुबह-सुबह ही ऐसे एक ज्ञानी ने दर्शन दिए। गीता उन्हें कंठस्थ है। चालीस वर्षों से गीता का पाठ करते हैं। अब सेवा से निवृत्त हुए हैं तो अहर्निश गीता का पारायण चल रहा है। उनकी बात-बात में गीता आ जाती है। चित्त को उसके शब्दों से खुद भर लिया है। प्रसंग हो या नहीं, उन शब्दों को दोहराते रहते हैं। बहुत अशांत हैं। कलह प्रिय हैं। जहां बैठते हैं वहीं विवाद कर बैठते हैं। लोग उनके ज्ञान से भय खाते हैं। उनके उपदेशों से बचते हैं। उनके हाथों में पड़ जाते हैं तो निकल जाते हैं। उन्हें कृष्ण के वचन समझ में आते हैं, लेकिन लोगों का उनके ज्ञान के प्रति जो भय है वह दिखाई नहीं देता। स्वयं की अशांति के कारण भी दिखाई नहीं देते, यद्यपि जगत में कैसे शांति होगी इसके लिए रामबाण नुस्खे वे अंगुलियों पर बता देते हैं। यह है शास्त्रों को, पराए विचारों को दोहराने वाले चित्त की जड़ता। ऐसे स्वयं की तो कोई समस्या हल नहीं होती है। और फिर जब अशांत चित्त व्यक्ति शास्त्रों को पकड़ लेते हैं तो शास्त्र भी संघर्ष, संगठन और हिंसा के कारण बन जाते हैं। क्या यह संभव है कि बुद्ध और क्राइस्ट, महावीर और जरथुस्त्र के शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने वाले बनें? क्या वे हिंसा और वैमनस्य के आधार हो सकते हैं? लेकिन चित्त की जड़ता उन्हें भी शोषण और संघर्ष, हिंसा और युद्ध में परिणत कर लेती है। धर्मों का इतिहास मनुष्य के मन की जड़ता के अतिरिक्त और किस बात की गवाही देता है?
- शास्त्रीय मस्तिष्क को मैं जड़ मस्तिष्क कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि जीवन की समस्याएं नित्य बदल जाती हैं, लेकिन उसके समाधान नहीं बदलते। दुनिया माक्र्स पर आ जावे तो भी वह मनु पर ही बैठा रहता है। फिर दुनिया माक्र्स से आगे निकल जाती है, लेकिन वह माक्र्स को ही पकड़ कर बैठ जाता है। बाइबिल छोड़ता है तो कैपिटल पकड़ लेता है, लेकिन बिना शास्त्र को पकड़े उसकी गति नहीं। जीवन को समझना उसे मूल्यवान नहीं मालूम होता। उसे तो सिद्धांतों और शब्दों से प्रेम होता है। यह भी इसलिए कि जीवन को समझने के लिए विचार चाहिए, जब कि शास्त्र को पकड़ने में विचार की कोई आवश्यकता नहीं। स्मृति को किसी भी चीज से भर लेना बड़ी सरल बात है, किंतु वह प्रौढ़ बुद्धि का लक्षण नहीं। प्रौढ़ता का लक्षण है विचार, समस्याओं को देखने की क्षमता। शास्त्रीय बुद्धि को समस्याएं दिखाई ही नहीं देतीं। समस्याएं तो उन खूंटियों की भांति होती हैं, जिन पर अपने बंधे-बंधाए, रटे-रटाए सिद्धांतों को टांगने में उसे मजा आता है। शास्त्रीय बुद्धि समस्या के अनुकूल समाधान नहीं, वरन अपने पूर्व-निर्धारित समाधान के अनुकूल ही समस्या को देखती है। और यह न देखने से भी बदतर है।
|
| 5V |
 |
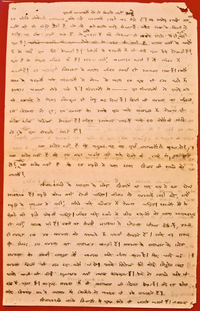 |
- क्योंकि इस भांति थोपे गए समाधान पुरानी समस्याओं को तो मिटाते नहीं, उलटे और नयी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। अप्रौढ़ दृष्टि उस पागल दर्जी की ही भांति होती है जो बने-बनाए कपड़े को खींचता है, और जब वे किसी के शरीर पर ठीक नहीं आते हैं तो उससे कहता है कि निश्चय ही आपके शरीर में ही कहीं कोई भूल है। पागल दर्जी के कपड़ों में कोई भूल कैसे हो सकती है? पंडितों के शास्त्रों में भी कोई भूल कैसे हो सकती है? भूल है तो जरूर जीवन में है, शास्त्रों में नहीं! बदलाहट करनी है तो जीवन में करनी है। इस जड़तापूर्ण चित्त-दशा के कारण जीवन व्यर्थ ही उलझता गया है। हजारों साल के शास्त्रों और परंपराओं के बोझ के कारण हम कुछ भी हल करने में क्रमश: असमर्थ होते गए हैं। परंपराओं ने..मृत परंपराओं ने..हमारे मन को सब ओर से घेर कर बिल्कुल ही पंगु कर दिया है। किसी भी समस्या का जीवंत हल खोजना तो दूर, उस समस्या को उसके मूल और नग्न रूप में देखना ही करीब-करीब असंभव हो गया है। जीवन उलझता जाता है और हम तोतों की भांति रटे हुए सूत्र दोहराते जा रहे हैं।
- क्या उचित नहीं है कि मनुष्य का मन मुर्दा समाधानों से मुक्त हो? क्या उचित नहीं है कि हम सदा अतीत की ओर देखने की दृष्टि से सावधान हों? और क्या उचित नहीं है कि हम स्मृति से ऊपर उठ कर विचार की शक्ति को जगावें?
- विचार-शक्ति के जागरण के लिए विचारों का भार कम से कम होना आवश्यक है। स्मृति बोझ नहीं होनी चाहिए। जीवन जो समस्याएं खड़ी करे, उन्हें स्मृति के माध्यम से नहीं, सीधे और वर्तमान में देखना चाहिए। शास्त्रों में देखने की वृत्ति छोड़नी चाहिए। जीवन और स्वयं के बीच शास्त्रों को लाना अनावश्यक ही नहीं, घातक भी है। स्वयं का संपर्क समस्या से जितना सीधा होता है, उतना ही ज्यादा हम उस समस्या को समझने में समर्थ हो जाते हैं। और वह समझ ही अंततः उस समस्या का समाधान बनती है। समस्या के समाधान के लिए समस्या को उसकी समग्रता में जानना और जीना पड़ता है। फिर चाहे वह समस्या किसी भी तल पर क्यों न हो। उसके विरोध में कोई सिद्धांत खड़ा करके कभी भी कोई सुलझाव नहीं लाया जा सकता, बल्कि व्यक्ति और भी द्वंद्व में पड़ता है। वस्तुतः समस्या में ही समाधान भी छिपा होता है। यदि हम शांत और निष्पक्ष मन से समस्या में खोजेंगे तो अवश्य ही उसे पा सकते हैं।
- विचार-शक्ति पराए विचारों से मुक्त होते ही जागने लगती है। जब तक
|
| 6 |
 |
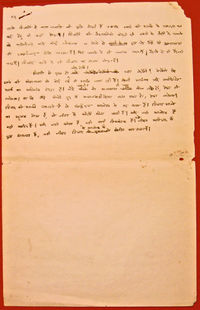 |
- पराए विचारों से काम चलाने की वृत्ति होती है तब तक स्वयं की शक्ति के जागरण का कोई हेतु ही नहीं होता। विचारों की बैसाखियां छोड़ते ही स्वयं के पैरों से चलने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न होने से मृत पड़े पैरों में अनायास ही रक्त-संचार होने लगता है। फिर चलने से ही चलना आता है।
- विचारों से मुक्त हों और देखें। क्या देखेंगे? देखेंगे कि स्वयं की अतःसत्ता से कोई नयी ही शक्ति जाग रही है। किसी अभिनव और अपरिचित ऊर्जा का आविर्भाव हो रहा है। जैसे च्रुहीन को अनायास ही च्रु मिल गए हों, ऐसा ही लगेगा; या जैसे अंधेरे गृह में अचानक ही दीया जल गया हो, ऐसा लगेगा। विचार की शक्ति जागती है तो अंतर्हृदय आलोक से भर जाता है। विचार-शक्ति का उदभव होता है तो जीवन में आंखें मिल जाती हैं। और जहां आलोक है, वहां आनंद है। और जहां आंख है, वहां मार्ग निष्कंटक है। जो जीवन अविचार में दुख हो जाता है, वही जीवन विचार के आलोक में संगीत बन जाता है।
|